सदीं के महान कवि व चरित्र निर्माता, गोस्वामी तुलसीदास जीकी उपरोक्त पंक्तियों की वर्तमान परिपेक्ष्य में प्रासंगिकता
डॉ प्रमोद कुमार
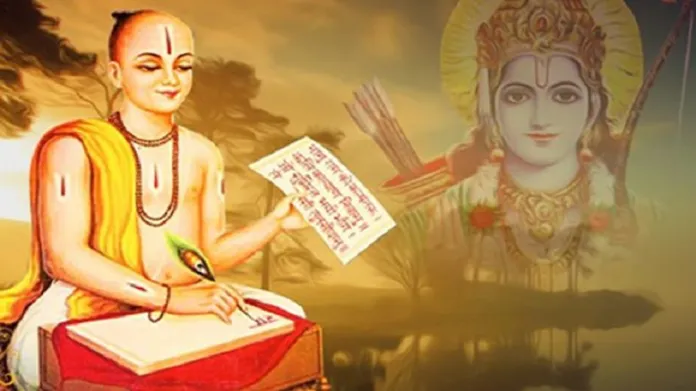
कि बंदऊं गुरु पद पदुम परागा I सुरुचि सुभाष, सरस अनुरागा
कि बंदऊं प्रथम महिसुर चरना I मोहि जनत, संसय सब हरना
सदीं के महान कवि व चरित्र निर्माता, गोस्वामी तुलसीदास जीकी उपरोक्त पंक्तियों की वर्तमान परिपेक्ष्य में प्रासंगिकता
गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित उपरोक्त दोहा भारतीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा में गुरु के महत्व को उजागर करता है। यह पक्तियां तुलसीदास जी द्वारा रचित “श्री रामचरितमानस” के आरंभ में कही गई हैं। इन पक्तियों में तुलसीदास जी अपने गुरु की वन्दना करते है।इस दोहे का भावार्थ गुरु महिमा का गुणगान करते हुए ज्ञान, भक्ति और जीवन की जटिलताओं को सुलझाने में उनके योगदान को रेखांकित करता है। तुलसीदास जी के शब्दों में ‘गुरु पद पदुम पराग’ अर्थात् गुरु के चरण कमलों की रज को वंदन करना न केवल आत्मिक उत्थान का मार्ग है, बल्कि मानव जीवन के समस्त संशयों को हरने का भी उपाय है।आज के आधुनिक युग में, जहाँ भौतिकवाद, व्यस्त जीवनशैली और सूचनाओं के अतिरेक ने मानसिक शांति को बाधित कर दिया है, गुरु की महिमा और उनका मार्गदर्शन पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। इस लेख में हम इस दोहे की विस्तृत व्याख्या करते हुए, गुरु की महत्ता, उनके प्रभाव, और वर्तमान समाज में इसकी प्रासंगिकता पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
गोस्वामी तुलसीदास जी एक महान कवि और चरित्र निर्माता थे, जिन्होंने हिंदी साहित्य में एक अमिट छाप छोड़ी। उनका जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था।तुलसीदास जी ने अपने जीवनकाल में कई महान कृतियों की रचना की, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध है “श्री रामचरितमानस”। यह एक महाकाव्य है जो भगवान राम की कहानी को बताता है और इसमें लगभग 12,000 छंद हैं।तुलसीदास जी की अन्य प्रसिद्ध कृतियों में “विनय पत्रिका”, “गीतावली”, “कवितावली”, और “दोहावली” शामिल हैं।तुलसीदास जी का प्रभाव हिंदी साहित्य और संस्कृति पर बहुत गहरा है। उनकी कविता ने हिंदी भाषा को समृद्ध बनाया और उन्हें हिंदी साहित्य के सबसे महान कवियों में से एक बनाया।तुलसीदास जी की मृत्यु 1623 में वाराणसी में हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद, उनकी कविता को और भी प्रसिद्धि मिली और वह हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण हिस्से बन गए।
दोहे की व्याख्या-
कि बंदऊं गुरु पद पदुम परागा
इस पंक्ति में तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं गुरु के चरण कमलों की धूल को वंदन करता हूँ। यहाँ ‘पद’का अर्थ चरण से है, ‘पदुम’का अर्थ कमल से है, और ‘पराग’का अर्थ पराग कण अर्थात् धूल से है। तुलसीदास जी गुरु के चरणों की धूल को भी अत्यंत पवित्र और मूल्यवान मानते हैं, क्योंकि यह ज्ञान, भक्ति और मुक्ति का स्रोत है।
गुरु न केवल ज्ञान के प्रदाता हैं, बल्कि वे आत्मिक चेतना के जागरण का मार्ग भी दिखाते हैं। भारतीय परंपरा में गुरु को माता-पिता से भी उच्च स्थान दिया गया है, क्योंकि वे जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझने में सहायता करते हैं।
सुरुचि सुभाष, सरस अनुरागा
इस पंक्ति में गुरु के गुणों का वर्णन किया गया है—
सुरुचि–गुरु की वाणी और उनके विचार सुरुचिपूर्ण होते हैं, व्यक्ति को सही मार्ग पर ले जाते हैं।
सुभाष– गुरु के शब्द कोमल, प्रभावशाली और ज्ञान से भरपूर होते हैं।
सरस अनुरागा–गुरु में सहज प्रेम और करुणा होती है, वे अपने शिष्यों के प्रति निःस्वार्थ प्रेम रखते हैं।गुरु केवल शाब्दिक ज्ञान नहीं देते, बल्कि अपने आचरण, प्रेम और मार्गदर्शन से शिष्य के हृदय में अध्यात्म और नैतिकता की स्थापना करते हैं।
कि बंदऊं प्रथम महिसुर चरना
यहाँ ‘महिसुर’का अर्थ है महा+ईश्वर अर्थात् श्रेष्ठ गुरु। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे सबसे पहले गुरु के चरणों की वंदना करते हैं। यह गुरु को ईश्वर के समकक्ष रखने का संकेत देता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में गुरु को ‘ब्रह्मा, विष्णु और महेश’ का स्वरूप माना गया है।
मोहि जनत, संसय सब हरना
गुरु का सबसे बड़ा कार्य शिष्य के संशयों को दूर करना होता है। अज्ञानता, असमंजस और मोह के कारण मनुष्य सही-गलत का निर्णय नहीं कर पाता, लेकिन गुरु उसे ज्ञान की रोशनी प्रदान कर इन बाधाओं को समाप्त करते हैं।
भारतीय संस्कृति में गुरु की भूमिका
गुरु-शिष्य परंपरा
भारतीय संस्कृति में गुरु-शिष्य परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। महाभारत में कृष्ण और अर्जुन का संवाद, उपनिषदों में ऋषियों का ज्ञानोपदेश, और गुरुकुल परंपरा इसके साक्षी हैं। तक्षशिला और नालंदा जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में भी गुरु को सर्वोच्च सम्मान था।
गुरु के चार प्रमुख स्वरूप
शिक्षक के रूप में गुरु–जो विद्या और ज्ञान प्रदान करते हैं।
मार्गदर्शक के रूप में गुरु–जो जीवन के कठिन मोड़ों पर सही दिशा दिखाते हैं।
आध्यात्मिक गुरु–जो आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझने में सहायता करते हैं।
प्रेरणास्रोत गुरु–जो अपने आचरण और जीवन से दूसरों को प्रेरित करते हैं।
आधुनिक युग में गुरु की प्रासंगिकता
शिक्षा में गुरु की भूमिका
आज के समय में शिक्षा प्रणाली पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक निर्भर हो गई है, जिससे नैतिक और व्यावहारिक शिक्षा की कमी हो रही है। डिजिटल माध्यमों से प्राप्त ज्ञान की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना कठिन होता जा रहा है। ऐसे में एक योग्य गुरु की आवश्यकता है जो न केवल सूचनाओं का संकलन कराए, बल्कि उनके सही प्रयोग की दिशा भी बताए।
आध्यात्मिक गुरु और मानसिक शांति
तेजी से भागती इस दुनिया में मानसिक तनाव, अवसाद और चिंता जैसी समस्याएँ बढ़ रही हैं। लोग जीवन में शांति और संतोष की खोज में हैं, परंतु उन्हें सही दिशा नहीं मिल पाती। यहाँ आध्यात्मिक गुरु की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, जो ध्यान, योग, और नैतिकता के माध्यम से व्यक्ति को आंतरिक शांति प्रदान कर सकते हैं।
डिजिटल युग में गुरु की नई परिभाषा
आज इंटरनेट और सोशल मीडिया के कारण हर व्यक्ति एक शिक्षक बन सकता है, लेकिन सच्चे गुरु की पहचान कठिन होती जा रही है। सही और गलत की पहचान के लिए भी एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है।
नैतिकता और चरित्र निर्माण
आज समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास देखा जा सकता है। लालच, असहिष्णुता, और अन्याय बढ़ रहे हैं। ऐसे में गुरु की भूमिका केवल ज्ञान देने तक सीमित नहीं रह जाती, बल्कि वे शिष्यों में अच्छे गुणों और आदर्शों का संचार भी करते हैं।
गुरु का महत्व – तुलसीदास से आज तक
तुलसीदास जी के समय में गुरु का महत्व केवल आध्यात्मिक उन्नति तक सीमित नहीं था, बल्कि वे समाज सुधारक, मार्गदर्शक और नैतिकता के संरक्षक भी थे। आज भी, यदि हम सही गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करें, तो न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि समाज में भी सुधार संभव है।
तुलसीदास जी का आदर्श गुरु
जो ज्ञान प्रदान करे और शिष्य के संशय दूर करे।
जो प्रेम और करुणा से भरपूर हो।
जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे।
आज का आदर्श गुरु
जो केवल पुस्तकीय ज्ञान न देकर व्यावहारिक शिक्षा भी दे।
जो आधुनिक समस्याओं का समाधान आध्यात्मिकता और तर्कसंगत दृष्टिकोण से दे।
जो नैतिकता और चारित्रिक विकास पर बल दे।
गोस्वामी तुलसीदास जी का यह दोहा न केवल भक्ति और अध्यात्म का संदेश देता है, बल्कि यह हमें जीवन में सही मार्गदर्शन की आवश्यकता का भी अहसास कराता है। आधुनिक युग में जहाँ भ्रम और तनाव ने व्यक्ति को अस्थिर कर दिया है, वहाँ सही गुरु का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है।गुरु केवल ज्ञानदाता नहीं होते, वे समाज के प्रकाश स्तंभ होते हैं। उनके बिना जीवन दिशाहीन हो सकता है। अतः, गुरु की महिमा को समझना और उनके मार्गदर्शन का सम्मान करना हर युग में आवश्यक है।

डॉ प्रमोद कुमार
डिप्टी नोडल अधिकारी, MyGov
डॉ भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा




