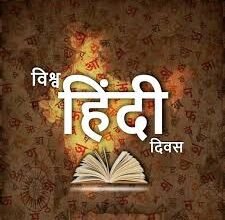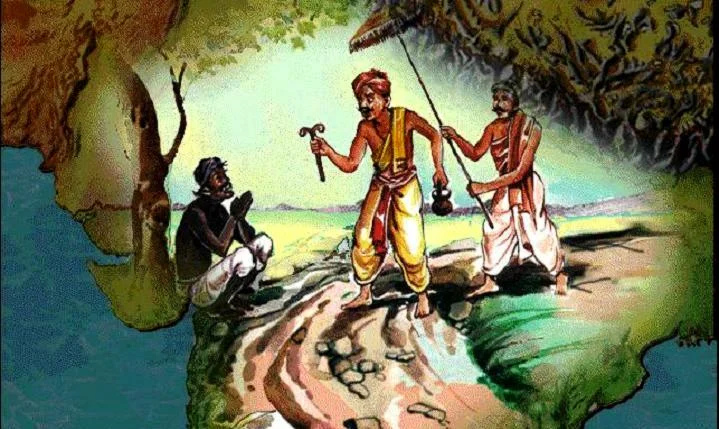
सनातन धर्म, जिसे ‘शाश्वत सत्य’ का वाहक माना जाता है, मूलतः आत्मा की एकता, करुणा, सहिष्णुता और वैश्विक बंधुत्व की भावना का पोषक रहा है। “वसुधैव कुटुम्बकम्” और “सर्वे भवन्तु सुखिनः” जैसे श्लोक इस धर्म के मूल स्वरूप में समता और सामाजिक समरसता के सिद्धांत को उजागर करते हैं।परंतु यथार्थ में, सनातन धर्म के नाम पर स्थापित सामाजिक संरचना जातिवादी व्यवस्था में बदल गई, जिसने समाज को जन्म आधारित श्रेणियों में बाँट दिया। प्रारंभिक वर्ण व्यवस्था जो गुण और कर्म पर आधारित थी, कालांतर में जन्म आधारित कठोर जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। यह व्यवस्था केवल सामाजिक असमानता नहीं, बल्कि धार्मिक अनुशासन के नाम पर मानसिक और शारीरिक गुलामी का माध्यम बन गई।
यह विरोधाभास—धर्म की एकता और जाति की विखंडनकारी सत्ता—भारत के धार्मिक और सामाजिक विकास में एक जटिल द्वंद्व के रूप में उपस्थित है। एक ओर उपनिषदों और भक्ति आंदोलन में आत्मा की समता की घोषणा होती रही, तो दूसरी ओर मनुस्मृति जैसी रचनाएँ जातिगत श्रेष्ठता और निम्नता को धार्मिक मान्यता देती रहीं। भारतीय समाज की सामाजिक संरचना को समझने के लिए सनातन धर्म और जाति व्यवस्था के संबंधों की विवेचना आवश्यक है। जहाँ एक ओर सनातन धर्म “वसुधैव कुटुम्बकम्”, “सर्वे भवन्तु सुखिनः” जैसी सार्वभौमिक एकता की अवधारणाओं को प्रकट करता है, वहीं दूसरी ओर जाति व्यवस्था एक कठोर सामाजिक श्रेणीकरण के रूप में उभरी जिसने समाज को खंडित किया।
“सनातन धर्म में जाति की सत्ता: धार्मिक एकता बनाम सामाजिक विभाजन” विषय का मूल द्वंद्व भारतीय समाज की उस गहरी विरासत को उजागर करता है जहाँ एक ओर ‘विविधता में एकता’ की अद्भुत मिसाल है, तो दूसरी ओर जातीय भेदभाव की विभाजनकारी दीवारें भी खड़ी हैं। सनातन धर्म की मूल आत्मा, ऋग्वेद से लेकर उपनिषदों तक, जीवन के विविध रंगों, विचारों और जीवन-शैलियों को स्वीकार कर एक समावेशी दृष्टिकोण को जन्म देती है। यहाँ नास्तिकता से लेकर अद्वैत वेदांत तक, भक्ति से लेकर कर्म मार्ग तक, सबको स्थान मिलता है—यानी विविधता को आत्मसात करने की अनुपम क्षमता। भारत की यह सांस्कृतिक विविधता ही उसकी आध्यात्मिक शक्ति रही है, जिसे सनातन धर्म ने पोषित किया। ‘सर्व धर्म समभाव’, ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ और ‘एकोऽहम् बहुस्यामि’ जैसे सिद्धांत धर्म के उस व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं जो हर जीव में एक ही ब्रह्म की अनुभूति करता है। यही भावना विविधताओं के बावजूद एकता की नींव है। परंतु जाति व्यवस्था, जो एक समय पर सामाजिक संगठन की आवश्यकता के रूप में उभरी थी, कालांतर में जन्माधारित सामाजिक भेदभाव और दमन का माध्यम बन गई। इसने धार्मिक एकता को आघात पहुँचाया और विविधता में जो एकता थी, उसे छिन्न-भिन्न कर दिया।
इस प्रस्तावना का उद्देश्य यह समझना है कि क्या सनातन धर्म की मूल भावना जातिगत भेदभाव की अनुमति देती है, या फिर यह एक सामाजिक विकृति है जो धर्म के मूल तत्व—करुणा, समता और सार्वभौमिक एकता—के विपरीत है। क्या सनातन धर्म का मूल स्वर जातिप्रथा को बढ़ावा देता है? क्या जातिगत विभाजन धर्म के उद्देश्य के अनुकूल है? यह लेख इसी विरोधाभास को गहराई से समझने और उसके ऐतिहासिक, धार्मिक, दार्शनिक एवं सामाजिक पहलुओं की विवेचना के लिए प्रस्तुत किया गया है। जब हम विविधता में एकता के आदर्श को केंद्र में रखकर जाति व्यवस्था का विश्लेषण करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि सच्चा सनातन धर्म विभाजन नहीं, बल्कि समरसता और समन्वय का प्रतीक है।
यह प्रस्तावना इस विमर्श की आवश्यकता को भी रेखांकित करती है कि हमें यह समझना होगा कि क्या जातिप्रथा वास्तव में सनातन धर्म का अभिन्न अंग है, या यह एक सामाजिक विकृति है जिसे धर्म का जामा पहनाया गया। इस विश्लेषण से न केवल धर्म का शुद्धिकरण संभव है, बल्कि एक समतामूलक, न्यायपूर्ण, विकसित, श्रेष्ठ और अखंड भारत की पुनर्रचना का मार्ग भी प्रशस्त हो सकता है।
1. सनातन धर्म की मूल अवधारणा
1.1. अर्थ और परिभाषा
“सनातन” का अर्थ है — ‘चिरंतन’, ‘शाश्वत’, ‘जो कभी समाप्त न हो’। अतः सनातन धर्म एक ऐसा दर्शन है जो समय की सीमाओं से परे है। यह कोई एक धर्म ग्रंथ या प्रवर्तक आधारित धर्म नहीं बल्कि विचारों, आस्थाओं और जीवन पद्धतियों का समुच्चय है।
1.2. वैदिक धर्म और सनातन धर्म
वैदिक काल के दौरान धर्म की अवधारणा कर्तव्यों, यज्ञ, ऋत और सत्य के पालन पर आधारित थी। किसी भी मनुष्य का मूल्यांकन उसके कर्मों के आधार पर होता था, जन्म के आधार पर नहीं।
2. जाति व्यवस्था की उत्पत्ति: पुरातन काल का दृष्टिकोण
2.1. वर्ण व्यवस्था बनाम जाति व्यवस्था
ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है — ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन गुण, स्वभाव और कर्मों पर आधारित था, न कि जन्म पर। भगवद्गीता (अध्याय 4, श्लोक 13) में कहा गया है: “चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः।” अर्थात चार वर्ण मैंने गुण और कर्म के आधार पर बनाए हैं। यह स्पष्ट करता है कि आरंभिक व्यवस्था में वर्ण लचीला था और व्यक्ति अपनी योग्यता से ऊपर या नीचे स्थान प्राप्त कर सकता था।
2.2. जाति व्यवस्था का विकास
कालांतर में यह वर्ण व्यवस्था कठोर जाति व्यवस्था में बदल गई। जातियाँ जन्म आधारित हो गईं और सामाजिक गतिशीलता रुक गई। यह परिवर्तन विशेषतः उत्तर वैदिक काल, स्मृति काल और मनुस्मृति जैसी ग्रंथों के प्रभाव से हुआ।
3. धर्म के माध्यम से सामाजिक एकता की अवधारणा
3.1. आध्यात्मिक दृष्टिकोण
सनातन धर्म का मूल संदेश आत्मा की एकता पर आधारित है। उपनिषदों में स्पष्ट रूप से कहा गया — “अहं ब्रह्मास्मि”, “तत्त्वमसि” — अर्थात सभी जीवों में वही ब्रह्म है।
3.2. भक्ति आंदोलन
संत कबीर, रविदास, तुलसी, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु आदि ने जाति विभाजन का विरोध करते हुए भगवान भक्ति को हर मनुष्य का अधिकार बताया। कबीर कहते हैं:
“जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान,
मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान।”
4. जातिप्रथा और धार्मिक ग्रंथों का संबंध
4.1. मनुस्मृति और जातिगत शास्त्रीय समर्थन
मनुस्मृति में जाति व्यवस्था को कठोर स्वरूप दिया गया — ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान, शूद्रों को निम्नतम। ये व्यवस्थाएं धार्मिक नहीं, सामाजिक सत्ता और वर्ग विशेष के वर्चस्व की देन थीं।
4.2. उपनिषद और समन्वय की दृष्टि
वहीं, उपनिषदों में एकात्मवाद और आत्मसाम्यता पर बल दिया गया। आत्मा को न कोई जाति होती है, न वर्ग। ये ग्रंथ जाति-निरपेक्ष हैं।
5. सामाजिक विभाजन के परिणाम और प्रभाव
5.1. मानसिक गुलामी और असमानता
जाति के आधार पर श्रेष्ठता-हीनता की भावना ने एक बड़े वर्ग को शिक्षा, ज्ञान, संपत्ति और अवसरों से वंचित रखा। इससे मानसिक गुलामी उत्पन्न हुई।
5.2. सामाजिक गतिशीलता का ह्रास
वर्ण से जाति में परिवर्तन के साथ ही सामाजिक गतिशीलता खत्म हो गई। एक व्यक्ति को जीवनभर एक ही पेशे में बाँध दिया गया।
6. जाति-धर्म संबंध पर ऐतिहासिक आलोचना
6.1. बुद्ध का विरोध
गौतम बुद्ध ने सनातन धर्म की जातिवादी विकृतियों का विरोध करते हुए एक नया मार्ग – धम्म का प्रतिपादन किया जो जाति-निरपेक्ष, तर्कसंगत और करुणा आधारित था। बुद्ध कहते हैं:
“न जात्या ब्राह्मणो होति, न जात्या होति अब्राह्मणो।”
(जन्म से कोई ब्राह्मण या अब्राह्मण नहीं होता)
6.2. महात्मा गांधी बनाम डॉ. अंबेडकर
गांधी ने ‘हरिजन’ कहकर जाति को सुधारने की बात की, जबकि डॉ. अंबेडकर ने इसे सामाजिक गुलामी का औजार मानते हुए इसका समूल नाश किया। उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, जो समता और करुणा पर आधारित था।
7. आधुनिक भारत में जाति की भूमिका
7.1. राजनीतिक लाभ और वोट बैंक
जाति एक राजनीतिक हथियार बन गई है। अनेक दल जाति आधारित वोट बैंक बनाकर सत्ता में आते हैं, जिससे सामाजिक समरसता बाधित होती है।
7.2. आरक्षण बनाम जातीय असमानता
आरक्षण की व्यवस्था सामाजिक असमानता दूर करने हेतु की गई थी, लेकिन इसका विरोध करने वाले तबके इसे जातिवाद का पुनर्जन्म मानते हैं, जबकि इसके पक्षधर इसे ऐतिहासिक न्याय की पुनर्प्राप्ति मानते हैं।
8. धार्मिक एकता का मार्ग: जातिविहीन सनातन धर्म की पुनर्रचना
8.1. मूल धर्म की ओर लौटना
सनातन धर्म की आत्मा — सत्य, करुणा, सेवा, एकात्मता — को पुनः जीवित कर जाति विभाजन से परे एक नया धार्मिक जीवन गढ़ा जा सकता है।
8.2. शिक्षा और विवेक
जातिगत सोच को नष्ट करने के लिए शिक्षा और आत्मबोध की आवश्यकता है। जब व्यक्ति खुद को आत्मा समझेगा, तब वह दूसरों को भी आत्मा के रूप में देखेगा — न कि जाति के चश्मे से।
9. वैकल्पिक दृष्टिकोण: नव-संवत्सर और नवधार्मिक चेतना
9.1. नव-संवत्सर की भूमिका
सनातन धर्म में नववर्ष के आगमन को आंतरिक शुद्धिकरण और आत्मा की उन्नति का अवसर माना गया है। यह समय जातिवाद के त्याग और समता के नए संकल्पों का भी है।
9.2. “नवधम्म” या समता आधारित धर्म
डॉ. अंबेडकर ने बौद्ध धम्म को “नवधम्म” के रूप में प्रस्तुत किया — जो जाति, पाखंड और अंधविश्वास से मुक्त था। ऐसे समतामूलक धर्म ही सनातन मूल्यों को जीवंत कर सकते हैं।
10. निष्कर्ष: जाति विहीन धर्म ही सच्चा धर्म
सनातन धर्म की आत्मा कभी जातिवादी नहीं रही। जाति व्यवस्था समाज की सत्ता संरचना की देन है, धर्म की नहीं। जब तक धर्म का नाम लेकर जाति आधारित भेदभाव जारी रहेगा, तब तक धर्म का स्वरूप विकृत रहेगा। हमें उस सनातन मूल की ओर लौटना होगा जहाँ “मानवता ही धर्म है”, जहाँ ब्राह्मणता का अर्थ ज्ञान और करुणा है, न कि जन्म से श्रेष्ठता। यह पुनरावलोकन केवल धार्मिक ही नहीं, सामाजिक और राष्ट्रीय उत्थान का भी आधार बनेगा।
सनातन धर्म की मूल आत्मा समावेश, सह-अस्तित्व और आध्यात्मिक एकत्व में निहित है, जबकि जाति व्यवस्था का वर्तमान रूप सामाजिक असमानता, भेदभाव और दमन का कारण बना हुआ है। वैदिक वाङ्मय, उपनिषद, गीता और भक्ति परंपरा—सभी में आत्मा की समानता, करुणा और समता पर बल दिया गया है, जहाँ किसी भी प्रकार के सामाजिक ऊँच-नीच को स्थान नहीं है। किन्तु ऐतिहासिक परिवर्तनों, राजनीतिक सत्ताओं और सामाजिक संरचनाओं के कारण जन्माधारित जाति व्यवस्था ने धर्म की इस मूल भावना को विकृत कर दिया।
सनातन धर्म ने जहाँ ‘अहं ब्रह्मास्मि’, ‘तत्त्वमसि’ जैसे महावाक्यों के माध्यम से आत्मिक एकता को प्रतिष्ठित किया, वहीं जातिवादी प्रवृत्तियाँ धार्मिक एकता को खंडित कर सामाजिक विघटन का माध्यम बनीं। यह विरोधाभास दर्शाता है कि धर्म का स्वरूप जब आध्यात्मिक रहा तब उसने समाज को जोड़ा, परंतु जब उसे जातिगत व्यवस्था से जोड़ा गया, तब उसने समाज में गहरी खाइयाँ उत्पन्न कीं। आज आवश्यकता इस बात की है कि सनातन धर्म के मूल तत्वों की पुनर्व्याख्या की जाए और जातिवादी व्याख्याओं से धर्म को मुक्त कर समतामूलक समाज की स्थापना की जाए। धार्मिक एकता की पुनर्स्थापना तभी संभव है जब सनातन धर्म को उसके मूल—अंतरात्मा की समानता, कर्म की प्रधानता और करुणा के आधार—पर पुनर्परिभाषित किया जाए। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सनातन धर्म स्वयं में जाति-आधारित विभाजन का पोषक नहीं, बल्कि विविधता में एकता का संवाहक है। वास्तविक धार्मिकता जातियों के नहीं, मनुष्यता के आधार पर समाज का निर्माण करती है।

डॉ प्रमोद कुमार
डिप्टी नोडल अधिकारी, MyGov
डॉ भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा