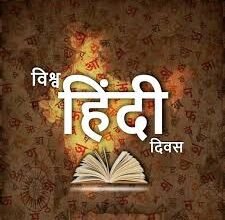भारतीय समाज में विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि दो परिवारों, संस्कृतियों और सामाजिक इकाइयों का समागम माना जाता है। यह संस्था हजारों वर्षों से सामाजिक व्यवस्था का एक केंद्रीय स्तंभ रही है। हालांकि, बदलते सामाजिक, आर्थिक और वैचारिक परिप्रेक्ष्य में विवाह संस्था और सामाजिक न्याय के बीच एक गहरा द्वंद्व उभर कर सामने आया है। एक ओर विवाह संस्था परंपरा, रीति-रिवाज और जातिगत सीमाओं पर आधारित है, तो दूसरी ओर सामाजिक न्याय समता, स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा के सिद्धांतों को प्राथमिकता देता है। भारतीय समाज की सबसे मजबूत और स्थायी संस्थाओं में से एक है वैवाहिक संस्था, जो पारंपरिक मूल्यों, रीति-रिवाजों और धार्मिक परंपराओं पर आधारित रही है।
वैवाहिक संस्था केवल दो व्यक्तियों के बीच संबंध नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक गठजोड़ का प्रतीक भी मानी जाती है। लेकिन जब हम इसे सामाजिक न्याय की दृष्टि से देखते हैं, तो इसके कई आयामों पर प्रश्नचिन्ह उठते हैं। क्या यह संस्था समानता, स्वतंत्रता और गरिमा जैसे न्यायसंगत मूल्यों का पालन करती है? या फिर यह असमानता, भेदभाव और पितृसत्ता को संस्थागत रूप से कायम रखती है? इस लेख में हम भारतीय वैवाहिक संस्था की गहराई से पड़ताल करेंगे—इसके ऐतिहासिक स्वरूप से लेकर वर्तमान परिवर्तन तक—और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों की कसौटी पर इसका विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे और साथ ही साथ भारतीय विवाह संस्था कैसे परंपरा में जकड़ी हुई है और कैसे सामाजिक परिवर्तन इसे चुनौती दे रहे हैं। इसका भी विस्तार से विश्लेषण करेंगे।
1. भारतीय विवाह संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
1.1 वैदिक काल में विवाह की धारणा
वैदिक काल में विवाह को ‘संस्कार’ माना गया था। यद्यपि उस समय विवाह में महिला की सहमति और शिक्षा का महत्व था, लेकिन धीरे-धीरे विवाह एक पितृसत्तात्मक और जाति आधारित संस्था में परिवर्तित हो गया।
1.2 मनुस्मृति और जातिगत व्यवस्था
मनुस्मृति जैसी ग्रंथों ने विवाह को सख्त जातिगत दायरे में बांध दिया। अंतर्जातीय विवाहों को निषिद्ध और अधार्मिक माना गया। इससे न केवल सामाजिक स्तरीकरण को बढ़ावा मिला, बल्कि सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का भी ह्रास हुआ।
1.3 मध्यकाल और धार्मिक संकीर्णता
मध्यकाल में विवाह में बाल विवाह, पर्दा प्रथा और सती जैसी अमानवीय प्रथाएं प्रचलित हुईं, जिसने महिलाओं की स्वतंत्रता और गरिमा को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया।
2. सामाजिक न्याय: अवधारणा और भारतीय परिप्रेक्ष्य
2.1 सामाजिक न्याय की परिभाषा
सामाजिक न्याय का तात्पर्य है – समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर, समान अधिकार और समान सम्मान प्रदान करना, चाहे वह किसी भी जाति, लिंग, धर्म, भाषा या वर्ग का हो।
2.2 संविधान में सामाजिक न्याय
भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय को एक मौलिक उद्देश्य माना गया है। अनुच्छेद 15, 16, 17, 21 जैसे प्रावधान नागरिकों को समानता और गरिमा प्रदान करते हैं।
2.3 विवाह संस्था और न्याय की टकराहट
जब विवाह केवल जाति, धर्म और पितृसत्तात्मक सोच पर आधारित हो, तो यह सामाजिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विरुद्ध हो जाता है।
3. परंपरा और विवाह: सामाजिक सीमाएं
3.1 जातिगत बंधन
विवाह आज भी अधिककतर समान जाति में होता है। अंतर्जातीय विवाह को आज भी कई समाजों में सम्मान नहीं मिलता और कई मामलों में ऑनर किलिंग तक होती है।
3.2 दहेज प्रथा
दहेज सामाजिक अन्याय का सबसे बड़ा प्रतीक है, जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा, अपमान और आर्थिक शोषण को जन्म देता है।
3.3 बाल विवाह
हालांकि यह कानूनन अपराध है, परंतु ग्रामीण और कुछ पिछड़े क्षेत्रों में आज भी यह जारी है।
3.4 महिला की भूमिका
पारंपरिक विवाह में महिला को आज्ञाकारी पत्नी, बहू और माँ के रूप में सीमित कर दिया जाता है, जिससे उसका व्यक्तित्व दबा रह जाता है।
4. परिवर्तन की लहर: आधुनिक भारतीय विवाह
4.1 शिक्षा और महिला सशक्तिकरण
शिक्षा और आत्मनिर्भरता ने महिलाओं को विवाह की पारंपरिक भूमिकाओं को चुनौती देने की ताकत दी है।
4.2 अंतर्जातीय और अंतर्धार्मिक विवाह
आज अधिक युवा अंतर्जातीय और अंतर्धार्मिक विवाह को स्वीकार कर रहे हैं, जिससे सामाजिक दीवारें टूट रही हैं।
4.3 न्यायिक हस्तक्षेप
सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों ने अंतर्जातीय विवाह को संवैधानिक संरक्षण देते हुए, पुलिस और समाज को अनुशासित करने के कई निर्णय दिए हैं।
4.4 समलैंगिक विवाह की बहस
LGBTQ+ समुदाय के अधिकारों को लेकर अब विवाह संस्था को पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
5. विवाह संस्था में सामाजिक न्याय की चुनौतियाँ
5.1 पितृसत्ता की गहरी जड़ें
अभी भी विवाह के बाद महिला को अपना घर, नाम, पहचान त्यागनी होती है। यह असमानता न्याय के विरुद्ध है।
5.2 परंपरा का अंधानुकरण
परंपरा के नाम पर ‘कुल-खानदान’, ‘खाप पंचायत’, और ‘सम्मान’ की अवधारणाएं सामाजिक अन्याय को बढ़ावा देती हैं।
5.3 विधिक सुधारों की सीमाएँ
कानून तो मौजूद हैं, परन्तु सामाजिक चेतना और जागरूकता के अभाव में उनका प्रभाव सीमित हो जाता है।
6. न्यायसंगत विवाह की ओर कदम
6.1 शिक्षा और संवाद
शिक्षा और खुला संवाद ही सामाजिक न्याय की नींव रख सकते हैं। विवाह को प्यार, सम्मान और स्वतंत्रता की भावना से जोड़ना होगा।
6.2 युवाओं की भूमिका
युवा वर्ग सामाजिक बेड़ियों को तोड़ते हुए एक न्यायपूर्ण समाज की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। उन्हें संवैधानिक मूल्यों को अपनाना होगा।
6.3 समाजिक संस्थाओं का समर्थन
NGO, बुद्धिजीवी वर्ग, मीडिया और न्यायपालिका को मिलकर विवाह संस्था के भीतर छिपे अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।
6.4 धर्म के मानवीय पक्ष को अपनाना
सभी धर्म प्रेम, करुणा और समानता की बात करते हैं। इन मूल्यों को विवाह संस्था में आत्मसात करना आवश्यक है।
7. विवाह और सामाजिक न्याय: अंतर्विरोध या समरसता?
विवाह संस्था को यदि केवल परंपरा के अनुसार चलाया जाएगा, तो यह सामाजिक न्याय से टकराव उत्पन्न करेगा। लेकिन यदि विवाह को दो स्वतंत्र व्यक्तियों के बीच का समझौता माना जाए, जिसमें समानता, गरिमा और स्वायत्तता हो, तो यह सामाजिक न्याय का एक माध्यम बन सकता है।
8. विवाह संस्था का पुनरावलोकन: न्यायसंगत दृष्टिकोण
8.1 विवाह को सामाजिक अनुबंध के रूप में देखना
विवाह को संस्कार से अधिक एक समान अधिकारों वाला अनुबंध माना जाना चाहिए, जिसमें दोनों पक्षों की सहमति और स्वतंत्रता सर्वोपरि हो।
8.2 विवाह कानूनों में संशोधन
समान नागरिक संहिता, समलैंगिक विवाह की मान्यता, दहेज निषेध कानून को प्रभावी बनाने जैसे कदम उठाने होंगे।
8.3 युवाओं को संवैधानिक मूल्य सिखाना
युवाओं को यह सिखाना होगा कि विवाह केवल सामाजिक स्वीकृति का मामला नहीं, बल्कि निजी स्वतंत्रता और समानता का अधिकार है।
9. विचारशील उदाहरण और केस स्टडी
9.1 डॉ. भीमराव अंबेडकर और उनका विवाह दृष्टिकोण
डॉ. अंबेडकर ने सामाजिक न्याय को अपने जीवन का मिशन बनाया। उन्होंने अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया और स्त्रियों के अधिकारों की पैरवी की।
9.2 लव जिहाद और सामाजिक ध्रुवीकरण
राजनीतिक और धार्मिक ध्रुवीकरण के चलते अंतर्धार्मिक विवाहों को ‘लव जिहाद’ जैसे शब्दों से जोड़ा गया, जो न्याय और स्वतंत्रता के विरुद्ध है।
9.3 ऑनर किलिंग की घटनाएं
हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अनेक जोड़ों को केवल इसलिए जान गंवानी पड़ी क्योंकि उन्होंने जातिगत या धार्मिक सीमाओं को लांघा।
10. भविष्य की राह: न्यायपूर्ण विवाह की कल्पना
10.1 विवाह की पुनर्परिभाषा
विवाह को एक समानता आधारित अनुबंध के रूप में देखना होगा न कि सामाजिक नियंत्रण के यंत्र के रूप में।
10.2 कानून और सामाजिक सुधार का संतुलन
केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, समाज में बदलाव लाने के लिए सामाजिक चेतना और व्यवहार परिवर्तन जरूरी है।
10.3 युवा नेतृत्व की भूमिका
विवाह के चुनाव में युवाओं को जाति, धर्म, वर्ग जैसे कारकों की बजाय प्यार, समझदारी और सम्मान को महत्व देना होगा। युवा ही राष्ट्र का नवनिर्माण करता है। समाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक प्रगति युवा की सोच समझ व सूझबूझ पर आधारित होती है। वर्तमान में युवाओं को समाजिक बंधनों व रूढ़िवादी सोच से मुक्त करना होगा ताकि वह अपनी सकारात्मक ऊर्जा को परिवार, समाज व राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक, रचनात्मक और सृजनात्मक दिशा में लगा सके। एक समृद्ध, सशक्त, अखंड और विकसित राष्ट्र निर्वाण हेतु युवाओं की सकारात्मक भागीदारी अतिआवश्यक है क्योंकि राष्ट्र का समुचित विकास युवा पीढ़ी पर आधारित होता है।
भारतीय वैवाहिक संस्था सामाजिक जीवन का एक प्रमुख आधार है, लेकिन इसे सामाजिक न्याय की कसौटी पर परखना आवश्यक हो गया है। यह संस्था जब तक जातिगत श्रेष्ठता, लिंग भेद, धार्मिक कट्टरता और आर्थिक शोषण पर आधारित रहेगी, तब तक यह असमानता और अन्याय का पोषण करती रहेगी। भारतीय विवाह संस्था और सामाजिक न्याय के बीच द्वंद्व एक गहरे सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक संघर्ष को दर्शाता है। परंपरा की बेड़ियाँ अगर सामाजिक न्याय के मार्ग में बाधक बनें, तो उन्हें तोड़ना आवश्यक है। विवाह संस्था को अगर मानवीय गरिमा, स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों पर पुनर्निर्मित किया जाए, तो यह केवल दो व्यक्तियों के मिलन की व्यवस्था नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम बन सकती है। अब समय है कि हम परंपरा और परिवर्तन के बीच संतुलन बनाते हुए एक न्यायपूर्ण और समानतामूलक समाज की दिशा में अग्रसर हों। हमें ज़रूरत है एक ऐसे समाज की, जहाँ विवाह दो बराबर व्यक्तियों के बीच प्यार, समझदारी और स्वतंत्रता का अनुबंध हो। विवाह संस्था को सामाजिक न्याय के सिद्धांतों – समानता, गरिमा, स्वतंत्रता और समावेशिता – के अनुरूप पुनर्गठित करना समय की मांग है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विवाह संस्था समाजिक न्याय पर आधारित है क्योंकि समाजिक न्याय की जागुरूकता शिक्षा के साथ प्रबल होती है। जैसे ही शिक्षा का विस्तार होगा वैसे ही समाजिक न्याय की जागुरूकता बढ़ेगी। आज यही कारण है कि वैवाहिक संस्था जैसी समाजिक रूठीवादी सोच से हटकर सामाजिक न्याय- समानता, स्वतंत्रता और स्वछंदता पर आधारित होती जा रही है। भौतिक आधुनिकता के साथ ही मानवीय सोच और स्वरूप भी आधुनिक रूप से समाजिक न्याय (समानता, स्वतंत्रता और स्वछंदता) को सहर्ष अपना रहा है। इसलिए वैवाहिक जीवन समाजिक न्याय पर ही आधारित व संचालित होना चाहिए इसी में परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवीय कल्याण है।

डॉ प्रमोद कुमार
डिप्टी नोडल अधिकारी, MyGov
डॉ भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा