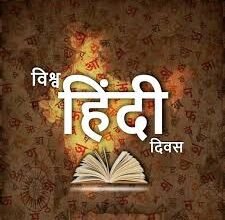“गुण बनाम जाति: गोस्वामी तुलसीदास और संत रैदास के विचारों में सामाजिक न्याय का द्वंद्व”
डॉ प्रमोद कुमार
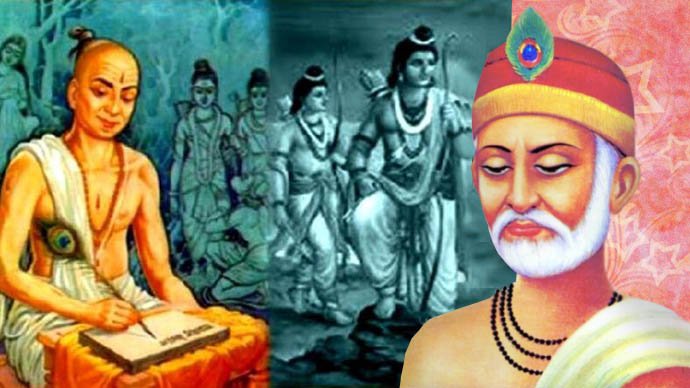
भारतीय समाज में जाति व्यवस्था ने सदियों से सामाजिक संरचना को दिशा दी है। यह व्यवस्था जन्म पर आधारित है, जो व्यक्ति के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थान को निर्धारित करती रही है। किंतु इस व्यवस्था के भीतर भी ऐसे चिंतनधारा विकसित हुई हैं जिन्होंने गुण, कर्म और आचरण को जाति से ऊपर रखा। भक्तिकालीन संतों ने विशेष रूप से इस द्वंद्व को अपने साहित्य, विचारों और जीवन के माध्यम से चुनौती दी। दो महान व्यक्तित्व—संत रैदास और गोस्वामी तुलसीदास इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। भारतीय समाज में सदियों से जाति व्यवस्था एक गहन और विवादास्पद विषय रही है। यह व्यवस्था सामाजिक संरचना को तय करने के साथ-साथ लोगों के जीवन, मान-सम्मान, और अधिकारों को भी प्रभावित करती रही है। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में अनेक संतों ने इस व्यवस्था को चुनौती दी, वहीं कुछ ने इसे अपरिहार्य सत्य की तरह स्वीकार भी किया।
इस लेख में हम दो महान संत-कवियों, गोस्वामी तुलसीदास और संत रैदास के विचारों की तुलना करेंगे, विशेषकर उनके उन उद्धरणों के माध्यम से, जिनमें जाति और गुण के आधार पर व्यक्ति की ‘पूज्यता’ पर बात की गई है। हालाँकि दोनों ने सामाजिक और धार्मिक विचारधारा में महान योगदान दिया, उनके दृष्टिकोण में जाति और गुण के प्रश्न पर स्पष्ट भिन्नता दिखाई देती है। रैदास जातिविहीन समाज की स्थापना के प्रबल पक्षधर थे, जबकि तुलसीदास, यद्यपि धार्मिक समरसता के समर्थक थे, पर जाति व्यवस्था को पूर्ण रूप से नकार नहीं सके। यही अंतर दोनों के विचारों में ‘गुण बनाम जाति’ के सामाजिक न्याय के द्वंद्व को जन्म देता है।
तुलसीदास का दृष्टिकोण:
“पूजहि विप्र सकल गुण हीना। शुद्र न पूजहु वेद प्रवीणा ॥”
गोस्वामी तुलसीदास, जो रामभक्ति की परंपरा के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, ने उपरोक्त दोहे में स्पष्ट रूप से यह विचार प्रस्तुत किया है कि जाति का स्थान गुण से ऊपर है। वे कहते हैं कि एक ब्राह्मण, भले ही सभी गुणों से रहित हो, तब भी पूजनीय है, जबकि एक शूद्र, चाहे वह वेदों का ज्ञाता ही क्यों न हो, पूज्य नहीं है। यह वक्तव्य तुलसीदास के समय की सामाजिक व्यवस्था और धर्मशास्त्रों से प्रभावित प्रतीत होता है। तुलसीदास धर्म के परंपरागत स्वरूप के पक्षधर थे, जिसमें वर्ण व्यवस्था को दिव्य और अपरिवर्तनीय माना गया था। उनके ग्रंथ रामचरितमानस में भी इस सामाजिक संरचना की पुष्टि मिलती है, जहां वह रामराज्य की परिकल्पना ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के अपने-अपने धर्मों का पालन करने में देखते हैं। यह दृष्टिकोण जन्म आधारित जातिव्यवस्था को समर्थन देता है और व्यक्ति की योग्यता या गुण की अपेक्षा उसकी जातिगत स्थिति को अधिक महत्व देता है।
रैदास का दृष्टिकोण:
“ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरणचंडाल के जो होवे गुण प्रवीन।”
दूसरी ओर, संत रैदास का यह दोहा जाति-आधारित भेदभाव को स्पष्ट रूप से नकारता है। वे एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत करते हैं — कि यदि कोई ब्राह्मण गुणहीन है, तो वह पूजनीय नहीं है, जबकि यदि कोई चांडाल (अंत्यज जाति का व्यक्ति) गुणवान है, तो वह पूजनीय है। यह वक्तव्य भक्ति आंदोलन के सामाजिक समता और व्यक्तिगत गुणों पर आधारित दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। रैदास स्वयं एक चर्मकार जाति से आते थे, जिन्हें उस समय समाज के सबसे निचले स्तर पर माना जाता था। उनके व्यक्तिगत अनुभवों ने उन्हें यह सिखाया कि जाति नहीं, बल्कि चरित्र, ज्ञान और भक्ति ही किसी व्यक्ति की सच्ची पहचान होते हैं। संत रैदास का यह विचार सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकार की भावना को दर्शाता है।
सामाजिक न्याय का द्वंद्व: जाति बनाम गुण
इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच जो अंतर है, वह केवल वैचारिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक, सामाजिक और नैतिक विमर्श का द्वंद्व भी है। तुलसीदास जहां वर्णाश्रम धर्म के अनुरूप व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, वहीं रैदास उस व्यवस्था की आंतरिक असमानताओं को उजागर कर उसे तोड़ने का प्रयास करते हैं। यह द्वंद्व इस सवाल को जन्म देता है — क्या व्यक्ति का मूल्यांकन जन्म से होना चाहिए या कर्म/गुण से? संत रैदास के उत्तर में सामाजिक न्याय की समावेशी दृष्टि है। उनका विचार कहता है कि सामाजिक सम्मान, पूजा या प्रतिष्ठा का मापदंड केवल गुण, सेवा, और मानवता होनी चाहिए।
भक्ति आंदोलन एक ओर समानता, सरल भक्ति और कर्म की महत्ता को बढ़ावा देता था, तो दूसरी ओर उसके कुछ संतों ने जाति व्यवस्था के भीतर रहते हुए ही भक्ति का मार्ग अपनाया। संत कबीर, संत रैदास, मीरा, आदि संतों ने जातिगत अहंकार और भेदभाव की खुलकर आलोचना की। तुलसीदास, सूरदास जैसे संतों ने परंपरागत सामाजिक संरचना को सीधा चुनौती नहीं दी, लेकिन उसमें रहते हुए भक्ति का मार्ग दिखाया। इससे स्पष्ट होता है कि भक्ति आंदोलन के भीतर भी जाति बनाम गुण का यह संघर्ष मौजूद था।
1. जाति व्यवस्था: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और सामाजिक संदर्भ
भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक उद्देश्य कार्य विभाजन था, किंतु कालांतर में यह जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गया। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र – चार प्रमुख वर्गों के अंतर्गत व्यक्ति को जन्म के आधार पर स्थान दिया गया। यह व्यवस्था ब्राह्मणवादी शास्त्रों, विशेषकर मनुस्मृति में स्पष्ट दिखाई देती है। शूद्रों और तथाकथित अछूतों को धार्मिक कर्मकांडों, शिक्षा, और मंदिर प्रवेश से वंचित किया गया। इस पृष्ठभूमि में जब रैदास और तुलसीदास का उदय हुआ, तब समाज जाति आधारित असमानता और सामाजिक अन्याय से ग्रसित था। दोनों संतों ने अपने-अपने ढंग से इन स्थितियों पर प्रतिक्रिया दी।
2. संत रैदास: जाति का अस्वीकार और गुण का उत्सव
संत रैदास, जिन्हें रविदास के नाम से भी जाना जाता है, 15वीं शताब्दी में वाराणसी में जन्मे थे। वे जन्म से चर्मकार जाति में उत्पन्न हुए, जो सामाजिक दृष्टि से अछूत मानी जाती थी। उन्होंने जाति व्यवस्था के विरुद्ध अपने विचारों और अनुभवों से एक क्रांतिकारी धारणा प्रस्तुत की।
2.1 प्रमुख विचार:
जाति नहीं, कर्म महत्वपूर्ण है:
“जाति-पाँति पूछे नहिं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई।”
रैदास ने स्पष्ट कहा कि ईश्वर की भक्ति में जाति का कोई स्थान नहीं। भक्ति के लिए केवल हृदय की पवित्रता चाहिए।
बेगमपुरा की संकल्पना: रैदास ने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहाँ न कोई जाति हो, न अन्याय, न दमन।
“ऐसा चाहूँ राज मैं, जहाँ मिले सबन को अन्न।”
“बेगमपुरा सहर को नाउँ॥ दुखु अँदोह नाहिं तिहि ठाउँ॥”
समानता का सिद्धांत: रैदास ने सवर्ण और अवर्ण के भेद को पूरी तरह नकार दिया। उनका मानना था कि सभी मनुष्य समान हैं, क्योंकि आत्मा एक है और ईश्वर भी एक है।
आत्मिक अनुभव पर बल: रैदास के अनुसार, व्यक्ति के भीतर ही ब्रह्म है। इस ब्रह्म की अनुभूति जाति से नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और समर्पण से होती है।
3. गोस्वामी तुलसीदास: धर्म आधारित सामाजिक व्यवस्था के समर्थक
गोस्वामी तुलसीदास, 16वीं शताब्दी के महान कवि और संत, रामचरितमानस के रचयिता थे। वे ब्राह्मण कुल में जन्मे और रामभक्ति के प्रखर प्रवक्ता थे। उनका धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण तुलनात्मक रूप से पारंपरिक था।
3.1 प्रमुख विचार:
वर्णाश्रम धर्म का समर्थन:
तुलसीदास ने मनुष्य के गुणों को महत्व देने की बात तो कही, लेकिन वर्ण व्यवस्था को भी स्वीकार किया:
“ब्राम्हण शूद्र नाग वन देवा। सबहि मोहि प्रिय प्रगट करि सेवा॥”
यहाँ सेवा करने पर सभी प्रिय हो सकते हैं, परंतु जन्म आधारित वर्गीकरण को अस्वीकार नहीं किया गया।
शूद्रों की स्थिति पर दृष्टिकोण:
“ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी। सकल ताड़ना के अधिकारी॥”
यह प्रसिद्ध पंक्ति तुलसीदास के दृष्टिकोण में जातिवादी और स्त्रीविरोधी मानसिकता का संकेत देती है। हालांकि आधुनिक विद्वानों में इस पंक्ति की व्याख्या को लेकर विभिन्न मतभेद हैं। धार्मिक समरसता का संदेश: तुलसीदास ने यह अवश्य कहा कि ईश्वर की भक्ति सबके लिए है, लेकिन सामाजिक पदक्रम में बदलाव की उन्होंने वकालत नहीं की।
रामराज्य की कल्पना:
रामराज्य उनके लिए आदर्श था, जिसमें शांति, समता और धर्म की प्रधानता थी। परंतु यह समता वर्णव्यवस्था के भीतर ही सीमित थी।
4. तुलसीदास बनाम रैदास: गुण और जाति का दार्शनिक द्वंद्व
4.1 दृष्टिकोण का अंतर:
जाति की अवधारणा जाति का निषेध वर्ण व्यवस्था का समर्थन गुणों का महत्व सर्वोपरि धार्मिक सेवा में गुण की प्रशंसा, पर जन्म के साथ संलग्न सामाजिक न्याय जातिविहीन समाज वर्णाश्रम में समरसता भक्ति मार्ग समता का मार्ग वर्ण व्यवस्था में समर्पण का मार्ग आदर्श समाज बेगमपुरा निष्कलंक, जातिविहीन रामराज्य धर्म आधारित सामाजिक अनुशासन
4.2 विचारों का टकराव:
रैदास गुण के आधार पर समाज की रचना करना चाहते थे, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान मिले। तुलसीदास गुणों की प्रशंसा तो करते हैं, लेकिन जन्म आधारित व्यवस्था को भी बनाए रखते हैं, जिससे सामाजिक न्याय सीमित हो जाता है।
5. सामाजिक न्याय की आधुनिक अवधारणा और इन दोनों दृष्टिकोणों की प्रासंगिकता
आधुनिक भारत में संविधान ने समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की स्थापना की है। जातिवाद के विरुद्ध कानून बनाए गए हैं और शिक्षा, अवसर, प्रतिनिधित्व आदि क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है।
5.1 रैदास के विचारों की प्रासंगिकता: आधुनिक संदर्भ में प्रासंगिकता
आज जब भारत सामाजिक न्याय, आरक्षण, समान अवसर, और जातिविहीन समाज की दिशा में बढ़ रहा है, तब यह द्वंद्व और अधिक प्रासंगिक हो उठता है। तुलसीदास का दृष्टिकोण आज की लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ प्रतीत होता है, क्योंकि वह जन्म के आधार पर व्यक्ति की स्थिति तय करता है। जबकि रैदास का विचार संविधान की मूल भावना के अनुरूप है, जो हर नागरिक को समान अधिकार, सम्मान और अवसर प्रदान करने की बात करता है।
आज शिक्षा, कार्यक्षमता, नैतिकता, सेवा भावना और करुणा को सामाजिक मान्यता का आधार बनाया जाना आवश्यक है, न कि जाति को। आज के लोकतांत्रिक भारत में रैदास का दृष्टिकोण अधिक समकालीन प्रतीत होता है। उन्होंने समानता, सामाजिक समरसता और जातिहीनता की कल्पना की, जो संविधान के मूल्यों से मेल खाती है।
5.2 तुलसीदास के योगदान की पुनर्व्याख्या:
तुलसीदास के रामायण ने धार्मिक चेतना को जनसाधारण तक पहुँचाया। उनके योगदान को साहित्य, धर्म और भाषा के क्षेत्र में अधिक महत्व दिया जा सकता है, जबकि सामाजिक दृष्टिकोण में उनकी सीमाएँ स्वीकारनी होंगी।
6. तुलसीदास और रैदास संवाद की कल्पना: गुण बनाम जाति पर विमर्श
कल्पना करें कि एक संवाद हो रहा है:
रैदास:
“तुलसी जी, क्या एक चर्मकार की आत्मा ईश्वर तक नहीं पहुँच सकती?”
तुलसीदास:
“रैदास जी, भक्ति सभी के लिए है, पर धर्म का अनुशासन वर्णों के अनुसार है।”
रैदास:
“तो क्या जन्म से ही कोई नीचा या ऊँचा हो सकता है? जब ईश्वर सबका है तो कोई अछूत कैसे हो सकता है?”
तुलसीदास:
“यह प्रश्न गंभीर है, किंतु समाज की स्थिरता के लिए व्यवस्था आवश्यक है।”
रैदास:
“व्यवस्था वह होनी चाहिए जो सबको समान अवसर दे, जाति नहीं, गुण हो आधार।”
“गुण बनाम जाति” का यह द्वंद्व भारतीय सामाजिक व्यवस्था की जड़ में बैठा हुआ है। संत रैदास और तुलसीदास दोनों ने अपनी-अपनी शैली में समाज को दिशा दी। जहाँ रैदास क्रांतिकारी थे, उन्होंने सामाजिक न्याय को केंद्र में रखा, वहीं तुलसीदास धार्मिक सौंदर्यशास्त्र के माध्यम से समरसता की कल्पना करते हैं, लेकिन वर्ण व्यवस्था की सीमाओं से मुक्त नहीं हो सके। “गुण बनाम जाति” का यह द्वंद्व सिर्फ तुलसीदास और रैदास के विचारों की तुलना नहीं है, यह भारतीय समाज के भीतर चल रही उस गहरी बहस का हिस्सा है, जो आज भी अनेक रूपों में जीवित है। जहां तुलसीदास जन्म के आधार पर सामाजिक पद और प्रतिष्ठा की स्थापना करते हैं, वहीं रैदास उस व्यवस्था को तोड़कर गुण आधारित न्याय और समता का मार्ग प्रशस्त करते हैं।
आज आवश्यकता इस बात की है कि हम संत रैदास के विचारों को आधुनिक सामाजिक और संवैधानिक मूल्यों से जोड़ें और एक ऐसे भारत की ओर अग्रसर हों, जहां व्यक्ति की पहचान उसके गुण, कर्म और मानवता से हो न कि उसकी जाति से। यह लेख इस यथार्थ को स्वीकार करने का आह्वान है “जाति से नहीं, गुण से बनती है पहचान।” इस प्रकार, सामाजिक न्याय के संदर्भ में रैदास का दृष्टिकोण समावेशी और आधुनिकता के अधिक निकट है। भारत के समतामूलक समाज के निर्माण में रैदास का दर्शन एक मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ के समान है।

डॉ प्रमोद कुमार
डिप्टी नोडल अधिकारी, MyGov
डॉ भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा