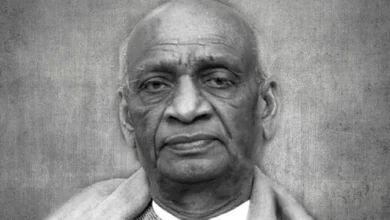“बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर का दर्शन: विचार और आचरण, समता-समानता का जीवन जीने की प्रेरणा व मार्ग, न कि राजनैतिक सत्ता पाने का हथियार”
डॉ प्रमोद कुमार

भारतीय इतिहास में ऐसे कुछ ही महापुरुष हुए हैं जिनकी दृष्टि केवल एक युग तक सीमित नहीं रही, बल्कि कालजयी बनकर मानवता के भविष्य का मार्गदर्शन करती रही। डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर ऐसे ही महामानव थे, जिनका जीवन किसी राजनीतिक पद या सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं था, बल्कि समाज में व्याप्त असमानता, अन्याय और शोषण के विरुद्ध एक विचार-आधारित क्रांति का प्रतीक था। वे केवल एक नेता या संविधान निर्माता नहीं थे, बल्कि विचार, कर्म और नैतिकता से ओतप्रोत एक जीवन-दर्शन के जीवंत प्रतिरूप थे। उनका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि समता-समानता और मानव गरिमा की स्थापना करना था।
बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर भारतीय समाज के उस उज्ज्वल युगपुरुष हैं जिन्होंने अपने विचार, आचरण और कर्म के माध्यम से मानवता, समता और सामाजिक न्याय की नई परिभाषा दी। उनका जीवन केवल राजनीति तक सीमित नहीं था, बल्कि वह एक वैचारिक आंदोलन और नैतिक जीवनशैली का प्रतीक था। आंबेडकर का लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि उस सत्ता संरचना को बदलना था जो सदियों से अन्याय, विषमता और भेदभाव पर टिकी हुई थी। उन्होंने भारतीय समाज को चेताया कि राजनीतिक स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब हर व्यक्ति को समान अवसर, समान सम्मान और समान अधिकार प्राप्त हों।
डॉ. आंबेडकर का दर्शन विचार और आचरण का संगम था। उन्होंने केवल समानता की बात नहीं की, बल्कि उसे अपने जीवन में जिया। अस्पृश्यता, जातिवाद और सामाजिक शोषण के विरुद्ध उनका संघर्ष यह दर्शाता है कि वे सत्ता नहीं, बल्कि समाज परिवर्तन के साधक थे। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि “शिक्षा ही मुक्ति का सबसे बड़ा साधन है।” इसलिए उन्होंने हर व्यक्ति को शिक्षित, संगठित और संघर्षशील बनने का आह्वान किया।
आज जब उनके नाम और विचारों का उपयोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया जा रहा है, तब यह आवश्यक है कि हम आंबेडकर को सत्ता की राजनीति से ऊपर उठकर एक विचार, प्रेरणा और जीवन-पद्धति के रूप में देखें। बाबा साहेब का दर्शन हमें यह सिखाता है कि सच्ची प्रगति तब ही संभव है जब समाज में समता, बंधुता और न्याय की स्थापना हो। वे वास्तव में सत्ता नहीं, बल्कि मानवता के सम्राट थे, जिनका जीवन स्वयं एक आदर्श मार्ग है।
1. आंबेडकर: विचारक, कर्मयोगी और सामाजिक क्रांतिकारी
डॉ. आंबेडकर ने भारतीय समाज की जड़ता, वर्णव्यवस्था और जाति-आधारित असमानताओं का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने समझा कि राजनीतिक आज़ादी तभी सार्थक होगी जब सामाजिक आज़ादी प्राप्त हो।
उनके विचारों की मूल प्रेरणा बुद्ध, कबीर, फुले और संत परंपरा से प्राप्त हुई थी। आंबेडकर का विश्वास था कि मनुष्य की मुक्ति ज्ञान, संगठन और संघर्ष के माध्यम से ही संभव है। इसलिए उन्होंने “शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो” का आह्वान किया।
यह नारा किसी पार्टी का घोष नहीं था, बल्कि मानव मुक्ति का शाश्वत संदेश था। डॉ. आंबेडकर ने अपनी पूरी जीवन यात्रा में सत्ता की नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की राजनीति की।
2. आंबेडकर का दर्शन: विचार और आचरण का अद्भुत संगम
डॉ. आंबेडकर का दर्शन केवल पुस्तकों में सीमित नहीं था, बल्कि उनके व्यवहार, कार्यों और निर्णयों में झलकता था। उनका जीवन “विचार को आचरण में बदलने” का प्रतीक था।
2.1 समता और समानता का सिद्धांत
उनका विचार था कि मनुष्य जन्म से नहीं, कर्म और आचरण से महान बनता है। उन्होंने ‘मनुस्मृति’ जैसी ग्रंथों की आलोचना इसलिए की, क्योंकि वे सामाजिक असमानता को स्थायी बनाते थे।
2.2 स्वतंत्रता का नैतिक अर्थ
डॉ. आंबेडकर के लिए स्वतंत्रता का अर्थ केवल राजनीतिक अधिकार नहीं, बल्कि आत्म-सम्मान और आत्मनिर्णय का अधिकार था। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति को अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने का अधिकार हो, चाहे वह धर्म, पेशा या विवाह से जुड़ा क्यों न हो।
2.3 भ्रातृत्व का महत्व
उन्होंने कहा — “फ्रेंच रेवोल्यूशन के नारे ‘स्वतंत्रता, समानता, बंधुता’ में से अगर बंधुता हटा दी जाए, तो अन्य दोनों बेअर्थ हो जाते हैं।”
उनके अनुसार बंधुता (Fraternity) सामाजिक एकता और नैतिक दायित्व का मूल आधार है।
3. डॉ. आंबेडकर का जीवन: सच्चे अर्थों में ‘विचार का कर्मरूप’
आंबेडकर का जीवन एक प्रयोगशाला था जिसमें उन्होंने अपने विचारों को कर्म के रूप में ढाला। वे जानते थे कि बिना शिक्षा और संगठन के कोई भी समाज स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने शिक्षण संस्थानों की स्थापना की, पत्रकारिता को जनजागरण का माध्यम बनाया, और अपने लेखन के माध्यम से समाज में चेतना फैलाई। उन्होंने कहा था
“मैं किसी से द्वेष नहीं रखता, लेकिन अन्याय के विरुद्ध समझौता भी नहीं कर सकता।”
उनका जीवन इस कथन का जीवंत उदाहरण था। चाहे उन्हें सामाजिक अपमान सहना पड़ा हो या राजनीतिक विरोध, उन्होंने अपने आदर्शों से कभी समझौता नहीं किया।
4. आंबेडकर और राजनीति: सत्ता नहीं, साधन के रूप में दृष्टि
डॉ. आंबेडकर ने राजनीति को समाज सुधार का माध्यम माना, न कि लक्ष्य।
उन्होंने स्पष्ट कहा था
“राजनीति मेरा अंतिम लक्ष्य नहीं है; मेरा लक्ष्य समाज को न्याय, समानता और बंधुत्व के मार्ग पर ले जाना है।”
4.1 संवैधानिक राजनीति
उन्होंने भारतीय संविधान की रचना केवल शासन के लिए नहीं, बल्कि एक नैतिक और सामाजिक परिवर्तन के उपकरण के रूप में की।
संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 21 आदि में समानता, भेदभाव-निषेध और जीवन के अधिकार के प्रावधान उनके विचारों की गहराई को दर्शाते हैं।
4.2 लोकतंत्र का अर्थ
उनके लिए लोकतंत्र केवल वोट डालने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन का एक तरीका (way of life) था।
उनका कहना था कि जब तक समाज में समानता और बंधुत्व स्थापित नहीं होते, तब तक लोकतंत्र केवल “राजनीतिक मुखौटा” रहेगा।
5. आंबेडकर का संघर्ष: समाज सुधार से धर्म परिवर्तन तक
डॉ. आंबेडकर का संघर्ष केवल अस्पृश्यता के विरुद्ध नहीं था, बल्कि मानव गरिमा की पुनर्स्थापना के लिए था।
5.1 शिक्षा के माध्यम से मुक्ति
उन्होंने कहा — “शिक्षा वह शस्त्र है जिससे आप संसार को बदल सकते हैं।”
उनकी दृष्टि में शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति नहीं, बल्कि चेतना का जागरण थी।
5.2 धर्म परिवर्तन का निर्णय
1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि केवल बौद्ध धर्म ही समता, करुणा और तर्कसंगतता पर आधारित है।
यह कदम किसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा नहीं, बल्कि उनके आत्मिक व नैतिक पुनर्जन्म का प्रतीक था।
6. आंबेडकर का समाजदर्शन: न्याय और करुणा की बुनियाद
उनके समाजदर्शन की जड़ें ‘न्याय’ और ‘करुणा’ में थीं। वे मानते थे कि
समाज में जब तक आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक समानता नहीं होगी, तब तक स्वतंत्रता अधूरी है।
जाति व्यवस्था न केवल सामाजिक अन्याय है, बल्कि मानवता के अपमान की पराकाष्ठा है।
उनके अनुसार भारत का पुनर्निर्माण तभी संभव है जब व्यक्ति का मूल्य उसके कर्म, ज्ञान और नैतिकता से तय किया जाए, न कि उसकी जाति या धर्म से।
7. आंबेडकर बनाम आधुनिक राजनीति
आज के राजनीतिक परिदृश्य में आंबेडकर के नाम और विचारों का प्रयोग सत्ता प्राप्ति के साधन के रूप में होने लगा है।
उनकी प्रतिमा, जयंतियाँ और घोषणाएँ राजनीतिक लाभ का माध्यम बन गई हैं, जबकि उनके सिद्धांत —
“समता, शिक्षित चेतना और मानवता” — पृष्ठभूमि में चले गए हैं।
डॉ. आंबेडकर ने चेताया था
“अगर मेरे नाम पर लोग केवल नारे लगाएंगे, लेकिन मेरे विचारों को नहीं समझेंगे, तो वह मेरे प्रति सबसे बड़ा अन्याय होगा।”
इसलिए आवश्यक है कि हम आंबेडकर को राजनैतिक प्रतीक नहीं, बल्कि वैचारिक मार्गदर्शक के रूप में देखें।
8. आंबेडकरवाद: जीवन जीने की प्रेरणा
आंबेडकरवाद का मूल सार है —
शिक्षा → आत्म-सम्मान → सामाजिक परिवर्तन।
यह विचारधारा मनुष्य को आत्मनिर्भर, तार्किक और नैतिक बनाती है।
आंबेडकरवाद का अभ्यास केवल राजनीतिक मंच पर नहीं, बल्कि
घर में समान व्यवहार,
समाज में सम्मानजनक संबंध,
शिक्षा में समान अवसर
और
शासन में पारदर्शिता
के रूप में होना चाहिए।
9. आंबेडकर की प्रासंगिकता: आज और कल
आज जब समाज फिर से वर्ग, धर्म और जाति के नाम पर विभाजित हो रहा है, तब आंबेडकर का विचार पहले से अधिक प्रासंगिक है।
उनका दर्शन हमें सिखाता है कि
विचार ही असली शक्ति है,
विनम्रता ही सच्चा नेतृत्व है,
समता ही सभ्यता का आधार है।
विकसित भारत तभी बनेगा जब प्रत्येक व्यक्ति आंबेडकर के जीवन-दर्शन को अपने आचरण में अपनाएगा, न कि केवल उनके चित्र को दीवार पर लगाएगा।
डॉ. भीमराव आंबेडकर केवल संविधान निर्माता नहीं थे, बल्कि भारत के नैतिक और वैचारिक निर्माता थे। उनका जीवन यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति सत्ता में नहीं, बल्कि विचार और आचरण की शुद्धता में निहित होती है। बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर का जीवन और दर्शन किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का परिणाम नहीं, बल्कि मानवता, समता और सामाजिक न्याय की एक जीवंत साधना था। उन्होंने अपने कर्म और चिंतन से यह सिद्ध किया कि विचार यदि कर्म में रूपांतरित हो जाए, तो वह समाज परिवर्तन का सबसे प्रभावी साधन बन जाता है। आंबेडकर ने राजनीति को सत्ता प्राप्ति का उपकरण नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाया। उनका लक्ष्य समाज के उस वर्ग को मुख्यधारा में लाना था, जिसे सदियों से अंधकार और अन्याय में रखा गया था।
उनका दर्शन यह सिखाता है कि जीवन का सच्चा अर्थ सत्ता नहीं, बल्कि समता है; पद नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा है; और जाति नहीं, बल्कि मानवता ही सर्वोपरि है। उन्होंने तर्क, ज्ञान और नैतिकता को जीवन की आधारशिला माना। आज जब आंबेडकर के नाम का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है, तब आवश्यक है कि हम उनके विचारों को कर्म में उतारें और उनके दिखाए मार्ग — शिक्षा, संगठन और संघर्ष — को अपने जीवन में अपनाएँ।
डॉ. आंबेडकर का जीवन एक प्रेरक संदेश देता है कि सच्ची क्रांति विचारों से जन्म लेती है, न कि सत्ता से। उन्होंने हमें सिखाया कि यदि समाज को विकसित और समान बनाना है तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर की असमानता, अज्ञान और अन्याय से संघर्ष करना होगा। इसलिए, बाबा साहेब केवल एक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि एक जीवन-दर्शन हैं — जो समता-समानता, नैतिकता और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। बाबा साहेब हमें यह मार्ग दिखाते हैं कि –
“विचार ही धर्म है, समता ही साधना है, और मानवता ही अंतिम लक्ष्य।”
अतः यह कहना उचित है कि – बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर का दर्शन एक जीवन शैली है, जो समता-समानता और मानव गरिमा का मार्ग दिखाता है — न कि सत्ता पाने का राजनैतिक हथियार।
डॉ प्रमोद कुमार
डिप्टी नोडल अधिकारी, MyGov
डॉ भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा