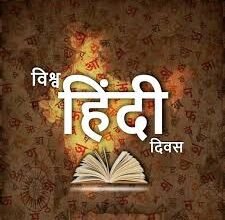“दलित: एक जाति नहीं, बल्कि शोषण के विरुद्ध चेतना और परिवर्तन की आवाज व संघर्षशील अस्मिता का प्रतीक”
डॉ प्रमोद कुमार

भारतीय समाज की सामाजिक संरचना बहुस्तरीय और जटिल रही है, जिसमें जातिव्यवस्था ने एक केंद्रीय भूमिका निभाई है। ‘दलित’ शब्द परंपरागत रूप से उन वर्गों के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिन्हें समाज की मुख्यधारा से बहिष्कृत, शोषित और अपमानित किया गया। परंतु यह शब्द केवल जातिसूचक नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत चेतना, संघर्ष, आत्मसम्मान और सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक बन चुका है। भारतीय समाज की सामाजिक संरचना में ‘दलित’ शब्द केवल एक जाति को परिभाषित नहीं करता, बल्कि यह उस ऐतिहासिक अन्याय, पीड़ा और बहिष्करण का प्रतीक है, जिसे सदियों से विभिन्न रूपों में झेला गया। दलित अस्मिता सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक शोषण की उस गाथा को प्रस्तुत करती है, जो न केवल सत्ता-संरचनाओं द्वारा निर्मित की गई, बल्कि उसे धर्म, परंपरा और नैतिकता के नाम पर वैधता भी प्रदान की गई।
“दलित” शब्द को जाति नहीं, बल्कि एक जीवित संघर्ष की प्रतीकात्मक पहचान के रूप में समझना आज के भारत की आवश्यकता है। यह सिर्फ उत्पीड़ितों का समूह नहीं, बल्कि शोषण के विरुद्ध उठती चेतना, बदलाव की ज्वाला और आत्मसम्मान की गर्जना है। भारत का इतिहास जहां वर्ण-व्यवस्था ने कुछ लोगों को देवत्व और बहुसंख्यकों को नीचता का दर्जा दिया, वहीं दलित चेतना इस अन्याय के विरुद्ध सैकड़ों वर्षों की चुप्पी को तोड़ती है।
वर्ण-व्यवस्था और मनुवादी सोच ने जिस भी वर्ग को ‘अस्पृश्य’ या ‘अवर्ण’ घोषित कर हाशिये पर डाला, वहीं से दलित चेतना की शुरुआत हुई—एक ऐसी चेतना जो अब शोषण के विरुद्ध परिवर्तन की प्रखर आवाज बन चुकी है। ‘दलित’ अब न केवल दमन का अनुभव है, बल्कि प्रतिरोध की विचारधारा, आत्मसम्मान की मांग और समानता की लड़ाई है। यह एक सामाजिक आंदोलन है, जो साहित्य, राजनीति, शिक्षा, संस्कृति और धर्म सभी क्षेत्रों में सशक्त उपस्थिति दर्ज करवा रहा है।
आज ‘दलित’ शब्द अपने मूल अर्थ को पार कर चुका है। वह उस संघर्षशील अस्मिता का प्रतिनिधित्व करता है, जो बहिष्कृत नहीं, बल्कि समावेशी भारत के निर्माण की मांग करता है। इस दृष्टिकोण से दलित एक क्रांतिकारी पहचान है—जो न्याय, गरिमा और समान अवसरों की स्थापना के लिए निरंतर गतिशील है। इसलिए यह आवश्यक है कि दलित को जाति की सीमाओं से परे एक समतामूलक चेतना और परिवर्तन की सामाजिक शक्ति के रूप में समझा जाए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दलित शब्द व्यापक रूप से विस्तृत किया गया है जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्तिओ जो किसी भी जाति, समाज, लिंग, अथवा धर्म से क्यों न हो इत्यादि को सम्मिलित किया है। यह लेख ‘दलित’ की जाति से परे एक व्यापक पहचान और विचारधारा के रूप में पड़ताल करता है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने की शक्ति निहित है।
2. ‘दलित’ शब्द का ऐतिहासिक और वैचारिक विकास
‘दलित’ का शाब्दिक अर्थ होता है – शोषित, पीड़ित, दबा हुआ, कुचला हुआ। यह शब्द प्राचीन संस्कृत साहित्य में भी मौजूद था लेकिन आधुनिक राजनीतिक-आलोचनात्मक अर्थों में इसका पुनर्जागरण ज्योतिराव फुले, डॉ आंबेडकर और दलित पैंथर्स के दौर में हुआ। ‘दलित’ शब्द में आत्मस्वीकृति, आत्मसम्मान, प्रतिरोध व बदलाव की चेतना है।
3. जाति नहीं, चेतना का प्रतीक: दलित की परिभाषा का पुनर्पाठ
दलित कोई जाति सूचक या जाति विशेष से नहीं बल्कि वे सभी लोग हैं जो ऐतिहासिक रूप से सामाजिक अन्याय, आर्थिक वंचना, सांस्कृतिक बहिष्कार और भौगोलिक हाशिये का शिकार रहे हैं। यह पहचान वर्गों, जातियों और क्षेत्रों की सीमाओं से परे है – यह अनुभव आधारित पहचान है।
4. सामाजिक शोषण की जड़ें: वर्णव्यवस्था और मनुस्मृति
मनुस्मृति और वर्णाश्रम धर्म ने ब्राह्मणवाद को वैचारिक संबल दिया और श्रम करने वाले को नीच बना दिया। दलितों को ‘अस्पृश्य’, ‘अपवित्र’ और ‘गृहहीन’ माना गया। सामाजिक शोषण इस व्यवस्था की रीढ़ बन गई, जिसमें मंदिरों में प्रवेश, कुओं से पानी भरना, स्कूलों में पढ़ना तक निषिद्ध था।
5. आर्थिक शोषण और संसाधनों से वांछित
दलितों को सदियों तक कृषि, भूमिहीनता, मजदूरी और बंधुआ मजदूरी तक सीमित रखा गया। भूमि-सुधार, आरक्षण, मनरेगा जैसे योजनाओं के बावजूद संसाधनों पर अधिकार का अभाव आज भी बना हुआ है। आज के कॉर्पोरेट भारत में दलित नवउदारवादी नीतियों के सबसे बड़े शिकार हैं।
6. सांस्कृतिक उपेक्षा और सांस्कृतिक प्रतिरोध
सांस्कृतिक इतिहास में दलितों को ‘असभ्य’, ‘संस्कृति-विहीन’ दिखाया गया, जबकि उन्होंने अपनी परंपराओं में लोकगीतों, नृत्य, धार्मिक रीति-रिवाजों और आस्था से भरे जीवन को जीवित रखा। तुलसी, कबीर, सूरदास, रैदास, मीरा व भक्तिकाल से लेकर आज उत्तराधुनिक के दलित कलाकारों और साहित्यकारों ने दलित शौषण के विरुद्ध सांस्कृतिक मोर्चा खोला।
7. भौगोलिक हाशिये पर: दलित बस्तियों की कहानी
भारत के हर गांव और शहर में दलितों को मुख्य समाज से दूर बसाया गया – ‘हरिजन बस्ती’, ‘नीची बस्ती’ जैसे नामों से उन्हें गेटो में समेटा गया। यह सिर्फ आवासीय विभाजन नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक बहिष्कार है, जो आज भी कायम है। शहरी स्लम और ग्रामीण दलित टोले इसकी गवाही देते हैं।
8. दलित आंदोलन: संगठित चेतना और सामाजिक क्रांति
फुले के सत्यशोधक समाज से लेकर डॉ. आंबेडकर के स्वतंत्रता संघर्ष और दलित पैंथर्स की क्रांति तक, दलित आंदोलन ने भारत की आत्मा को झकझोरा। यह आंदोलन सिर्फ दलितों के लिए नहीं, बल्कि समता, न्याय और मानवता के लिए लड़ा गया आंदोलन था।
9. डॉ. आंबेडकर और दलित अस्मिता का पुनर्निर्माण
डॉ. भीमराव आंबेडकर ने ‘मैं हिंदू पैदा हुआ, पर हिंदू नहीं मरूंगा’ कहकर दलित मुक्ति को धार्मिक पुनर्जागरण से जोड़ा। उन्होंने संविधान के माध्यम से समता और न्याय का रास्ता खोला, दलित अस्मिता को वैश्विक मंच दिया और शिक्षा को मुक्ति का औजार बनाया।
10. दलित साहित्य: अनुभव, प्रतिरोध और परिवर्तन
दलित साहित्य आत्मकथा की तरह है – अनुभव की कसमसाहट से उपजा। ओमप्रकाश वाल्मीकि, शरणकुमार लिंबाळे, बामा, गुनासेकरन, श्यामलाल, कुसुम मेहदल, शीलाबाई, बामा, रजनी तिलक, मोहनदास नेमीशरण, स्वराज सिंह बेचैन जैसी आवाज़ें सामाजिक यथार्थ की वह तस्वीर पेश करती हैं, जिसे मुख्यधारा अक्सर छिपा देती है।
11. दलित स्त्री: दोहरी मार और दुहरी चेतना
दलित स्त्रियाँ सामाजिक, लैंगिक और जातिगत शोषण की त्रिस्तरीय पीड़ा झेलती हैं। बलात्कार, अपमान, अशिक्षा और आर्थिक पराधीनता ने उनके अस्तित्व को चुनौती दी, लेकिन उन्होंने भी संघर्ष और नेतृत्व में भूमिका निभाई – बीनादास, रजनी तिलक, उषा रमण, कविता भट्ट जैसे उदाहरण इसका प्रमाण हैं।
12. समकालीन भारत में दलित विरोध और सत्ता-संघर्ष
आज भी उना, हाथरस, भीमा कोरेगांव, सहारनपुर जैसे कांडों से स्पष्ट होता है कि दलित चेतना को सत्ता-पोषित ताकतें दबाना चाहती हैं। शिक्षा, स्वास्थ, रोजगार, प्रतिनिधित्व और सम्मान – इन चारों मोर्चों पर दलित संघर्ष जारी है।
13. दलित राजनीति: चेतना से प्रतिनिधित्व की ओर
बसपा, रिपब्लिकन पार्टी, दलित पैंथर्स से लेकर अनेक स्थानीय संगठनों तक, दलित राजनीति अब केवल सत्ता नहीं, विचार और नीति का प्रश्न बन चुकी है। हालांकि जातिगत समीकरणों में वह कई बार कमजोर पड़ जाती है, लेकिन वह राजनीतिक विमर्श को निर्णायक दिशा दे रही है।
14. शिक्षा, न्याय और दलितों की सामाजिक प्रगति
शिक्षा और न्याय ही दलित मुक्ति की धुरी हैं। विश्वविद्यालयों में आरक्षण के बावजूद भेदभाव, आत्महत्याएँ, टोकनिज्म और जातिवादी मानसिकता एक बड़ी चुनौती हैं। लेकिन अश्वत्थामा, तुलसीराम, रोहित वेमुला जैसे नाम प्रेरणा देते हैं।
15. दलित और बौद्ध धम्म: आत्म-सम्मान की यात्रा
डॉ. आंबेडकर ने बौद्ध धर्म को दलितों की मुक्ति का मार्ग बताया। धम्म में समता, करुणा और बुद्धत्व का मूल्य है – वह ब्राह्मणवाद के तम को खंडित करता है। आज लाखों दलित बौद्ध रूपांतरण के माध्यम से एक नई वैचारिक दुनिया का निर्माण कर रहे हैं।
16. मीडिया, सिनेमा और दलित छवियों की राजनीति
मुख्यधारा का मीडिया दलित मुद्दों को या तो हाशिये पर रखता है या अपराध और करुणा तक सीमित करता है। लेकिन ‘जय भीम’, ‘फैंड्री’, ‘आर्टिकल 15’, ‘सैराट’ जैसे प्रयासों ने दलित अनुभव को दृश्यता दी है। वैकल्पिक मीडिया प्लेटफॉर्म अब दलितों की सशक्त आवाज़ बन रहे हैं।
17. सामाजिक न्याय की दिशा में संविधानिक प्रयास
भारत का संविधान – विशेषकर अनुच्छेद 15, 17, 46 – दलितों को सुरक्षा और अवसर देने का संवैधानिक ढांचा प्रस्तुत करता है। आरक्षण, प्रमोशन, स्कॉलरशिप, विशेष कानून – ये सब बदलाव के औजार हैं। लेकिन सही क्रियान्वयन और मानसिक बदलाव अब भी दूर हैं।
18. दलित अस्मिता और नवचेतना की वैश्विक ध्वनि
दलित आंदोलन अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं। अमेरिका, यूके, जापान में दलित संगठन सक्रिय हैं। संयुक्त राष्ट्र में दलित उत्पीड़न पर चर्चा होती है। यह वैश्विक मानवाधिकार का विषय बन चुका है – “Cast in India, but not destined to be casteless.”
19. चुनौतियाँ शेष हैं: नव-शोषण के आधुनिक रूप
आज जाति सीधे नहीं बोलती – वह छद्म रूप में मौजूद है। ‘योग्यता’ के नाम पर आरक्षण विरोध, ‘क्लीन इंडिया’ के नाम पर सफाई काम में दलितों की भरती, ‘मेरिट’ के नाम पर संस्थानों में भेदभाव – ये नए शोषण हैं, जो पुराने ढांचे को ही पोषित करते हैं।
20. दलित: नवभारत का पथप्रदर्शक
दलित कोई सामाजिक श्रेणी नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की आत्मा है। वह प्रश्न है, उत्तर भी। वह पीड़ा है, समाधान भी। जब तक भारत में दलितों को सम्मान, अधिकार और गरिमा नहीं मिलेगी, तब तक लोकतंत्र अधूरा रहेगा।
दलित कोई संकुचित जातिगत पहचान नहीं, बल्कि भारतीय समाज की वह ऐतिहासिक पीड़ा है, जिसे सदियों से सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक स्तर पर योजनाबद्ध रूप से दबाया गया। किंतु यह पीड़ा अब मात्र करुणा नहीं, प्रतिरोध की चेतना और बदलाव की प्रखर आवाज बन चुकी है। ‘दलित’ शब्द अब दया की याचना नहीं, गरिमा की घोषणा है। यह उस संघर्षशील अस्मिता की पहचान है, जो जाति आधारित शोषण के विरुद्ध खड़ी होकर समता, न्याय और स्वाभिमान की राह पर अग्रसर है।
आज दलित चेतना साहित्य में, राजनीति में, धर्म में, शिक्षा में और सामाजिक आंदोलनों में क्रांति का रूप धारण कर चुकी है। डॉ. आंबेडकर की विचारधारा, बौद्ध धम्म की करुणा, दलित साहित्य का यथार्थ, दलित स्त्रियों की दुहरी मुक्ति की आकांक्षा—यह सब मिलकर उस नवभारत की नींव रख रहे हैं, जहां किसी को सिर्फ उसके जन्म या जाति के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकेगा।
इसलिए यह अत्यावश्यक है कि ‘दलित’ को केवल जाति की दृष्टि से नहीं, बल्कि एक वैचारिक आंदोलन, चेतनात्मक परिवर्तन और मानव गरिमा के संघर्ष के रूप में देखा जाए। जब तक समाज में समता, न्याय और आत्मसम्मान की पूर्ण स्थापना नहीं होती, तब तक ‘दलित’ अस्मिता की यह आवाज चुप नहीं होगी। यही आवाज विकसित, समान और समरस भारत की असली ध्वनि है। दलित अस्मिता का संघर्ष सिर्फ उनके लिए नहीं, समूचे भारत के लिए है – एक समतामूलक, न्यायपूर्ण, संवेदनशील राष्ट्र के निर्माण हेतु।

डॉ प्रमोद कुमार
डिप्टी नोडल अधिकारी, MyGov
डॉ भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा