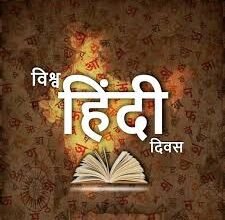“स्त्री पैदा नहीं होती, बनायी जाती है” – सिमोन द बोउवार के कथन की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता और महत्व
डॉ प्रमोद कुमार

“स्त्री पैदा नहीं होती, बनायी जाती है” — यह कथन बीसवीं सदी की प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक, लेखिका और स्त्रीवादी विचारक सिमोन द बोउवार (Simone de Beauvior) की अमर कृति The Second Sex का सार है, जिसने स्त्री-विमर्श की धारा को एक नया आयाम प्रदान किया। यह वाक्य मात्र एक वाक्य नहीं, बल्कि एक चुनौती है उस परंपरागत सोच को, जो स्त्री की पहचान को जैविक सीमाओं में बाँधकर देखती रही है। सिमोन का यह कथन स्पष्ट करता है कि स्त्रीत्व कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से गढ़ा गया चरित्र है। जन्म से लेकर मृत्यु तक स्त्री को ‘स्त्री’ बनाने की प्रक्रिया समाज, धर्म, संस्कृति और शिक्षा के माध्यम से संचालित होती है। यह कथन स्त्रीत्व की जैविक व्याख्या के विरुद्ध जाकर यह दावा करता है कि स्त्रीत्व एक सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक निर्माण है। यह कथन स्त्रीवाद के इतिहास में एक मील का पत्थर है, जिसने आधुनिक स्त्रीवादी विमर्श की दिशा ही बदल दी। आज जब हम लैंगिक समानता, लैंगिक पहचान, पितृसत्ता, सामाजिक-राजनीतिक सहभागिता और सांस्कृतिक रूढ़ियों पर बात करते हैं, तब यह कथन और भी अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है। यह न सिर्फ स्त्रियों की स्थिति को समझने में सहायक है, बल्कि उसे बदलने की दिशा भी देता है।
समाज ने स्त्री की भूमिका को ‘पत्नी’, ‘माँ’, ‘त्यागमयी’, ‘कोमल’ जैसे पूर्वनिर्धारित खांचों में बाँध दिया है, जिससे उसकी स्वतंत्रता, निर्णय शक्ति और आत्मनिर्भरता प्रभावित होती है। इस कथन के माध्यम से बोउवार यह उजागर करती हैं कि स्त्री एक ‘दूसरे’ के रूप में परिभाषित की गई है — वह जो पुरुष की तुलना में है, न कि स्वयं में एक स्वतंत्र सत्ता। यह विचार आज के सामाजिक परिदृश्य में भी उतना ही प्रासंगिक है, जहाँ एक ओर स्त्रियाँ चाँद तक पहुँच रही हैं, वहीं दूसरी ओर उनके अस्तित्व को अब भी परंपरा, नैतिकता और यौनिकता की सीमाओं में बाँधा जा रहा है। इस प्रस्तावना में हम इस ऐतिहासिक कथन के सामाजिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक आयामों की पड़ताल करेंगे तथा वर्तमान भारत सहित वैश्विक संदर्भों में इसकी प्रासंगिकता और संभावनाओं पर विचार करेंगे। यह विषय आज की पीढ़ी के लिए आत्ममंथन और सामाजिक पुनर्रचना का आह्वान है।
1. ऐतिहासिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि
1.1 सिमोन द बोउवार और ‘द सेकंड सेक्स’
The Second Sex एक दार्शनिक और समाजशास्त्रीय ग्रंथ है, जो यह विश्लेषण करता है कि किस प्रकार समाज ने स्त्री को “अन्य” (Other) के रूप में देखा है – पुरुष की प्राथमिकता और स्त्री की द्वितीयता को स्थापित करते हुए। बोउवार का यह कथन एक्ज़िसटेन्शियलिज्म की सोच से प्रेरित है, जहाँ अस्तित्व (existence) और सार (essence) के बीच फर्क किया जाता है – यानी स्त्री पैदा नहीं होती, बल्कि उसे सामाजिक रूप से “स्त्री” के रूप में गढ़ा जाता है।
सिमोन द बोउवार ने यह कथन अपनी पुस्तक The Second Sex (1949) में प्रस्तुत किया। इस पुस्तक में उन्होंने यह तर्क दिया कि स्त्री का “स्त्रीत्व” कोई प्राकृतिक, जन्मजात अवस्था नहीं है, बल्कि यह समाज द्वारा थोपा गया एक निर्माण है। मुख्य विचार: जैविक भिन्नता (महिला और पुरुष के शारीरिक अंतर) को स्त्री और पुरुष के सामाजिक, नैतिक और बौद्धिक अंतर का आधार नहीं बनाया जा सकता। स्त्री का व्यक्तित्व, उसकी पहचान और उसकी भूमिका – ये सब समाज, परंपरा, धर्म, संस्कृति और पितृसत्ता के माध्यम से गढ़े जाते हैं। यह विचार Existentialism (अस्तित्ववाद) से प्रेरित है, जिसमें व्यक्ति की पहचान उसके कृत्य और समाज में उसके अनुभवों से बनती है, न कि केवल जन्म से।
1.2 जैविक बनाम सामाजिक पहचान
सामान्यत: “स्त्री” को एक जैविक श्रेणी माना जाता है – अर्थात् जो महिला जननांगों के साथ जन्म लेती है, वही स्त्री कहलाती है। लेकिन बोउवार कहती हैं कि जैविक स्त्रीत्व अपने आप में ‘स्त्री’ की पहचान नहीं है। ‘स्त्री’ बनना एक सामाजिक प्रक्रिया है – जिसे शिक्षा, संस्कृति, भाषा, धर्म और पारिवारिक मानदंड गढ़ते हैं।
2. सामाजिक निर्माणवाद और लैंगिक पहचान
2.1 समाज द्वारा थोपे गए स्त्रीत्व के मानदंड
बचपन से ही लड़कियों को “नाजुक,” “शालीन,” “त्यागी,” और “सहनशील” बनने की सीख दी जाती है। खिलौनों से लेकर परिधान, भाषा, व्यवहार, करियर विकल्प और यहां तक कि इच्छाएं भी लिंग के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। लड़कियों को गुड़िया दी जाती है, जबकि लड़कों को बंदूकें और गाड़ियाँ। यह अंतर धीरे-धीरे उनकी भूमिका को परिभाषित करने लगता है।
2.2 विद्यालय, मीडिया और धर्म की भूमिका
विद्यालयों में लिंग आधारित अपेक्षाएं: अध्यापक लड़कों से नेतृत्व की उम्मीद करते हैं, जबकि लड़कियों से अनुशासन और आज्ञाकारिता की।
मीडिया में स्त्रियों को प्रायः सौंदर्य और शरीर की वस्तु के रूप में दिखाया जाता है – “आदर्श स्त्री” वह है जो सुंदर, पतली, सजी-संवरी हो।
धार्मिक परंपराएं स्त्री को पतिव्रता, त्यागमयी, गृहलक्ष्मी जैसे विशेषणों से बाँधती हैं, जिससे स्त्रीत्व का एक संकीर्ण फ्रेम तैयार होता है।
3. स्त्री का सामाजिक निर्माण: पितृसत्ता की भूमिका
इस कथन का मूल भाव यह है कि स्त्री का स्त्री होना एक जैविक तथ्य नहीं, सामाजिक प्रक्रिया है। पितृसत्तात्मक समाज एक लड़की को जन्म से ही इस प्रकार गढ़ने लगता है कि वह ‘स्त्री’ बन जाए – एक ऐसी पहचान जो उसे पुरुष की अपेक्षा में हीन, निर्भर, कोमल और त्यागमयी बनाती है।
उदाहरण: बचपन से लड़कियों को गुड़ियों से खेलना, सुंदरता की चिंता करना, घरेलू कामों में रुचि लेना सिखाया जाता है। नारीत्व को त्याग, शील, सहनशीलता, सादगी आदि गुणों से जोड़ा जाता है – जो समाज द्वारा तैयार की गई ‘आदर्श स्त्री’ की छवि है।
निष्कर्ष: समाज स्त्रियों को ऐसे रोल में ढालता है जिससे वे स्वतंत्र रूप से सोचने और निर्णय लेने की शक्ति से वंचित रह जाएं।
4. शिक्षा, धर्म और संस्कृति की भूमिका
शिक्षा, धर्म और सांस्कृतिक धारणाएं इस सामाजिक निर्माण को वैधता प्रदान करती हैं।
शिक्षा: पाठ्यक्रमों और सामाजिक वातावरण के माध्यम से लड़कियों को यह सिखाया जाता है कि उनकी भूमिका परिवार और गृहस्थी तक सीमित है।
धर्म: स्त्री को देवी भी कहा जाता है और पाप का मूल भी – यह द्वैत उसे एक बंधन में जकड़ देता है।
संस्कृति: साहित्य, फिल्मों, लोककथाओं आदि में स्त्री की छवि अक्सर दया, त्याग, सेवा या भोग्या के रूप में दिखाई जाती है।
नतीजा: स्त्री के बारे में सांस्कृतिक सोच उसकी स्वतंत्रता और व्यक्तित्व के विरुद्ध काम करती है।
5. मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव
जब स्त्री को बार-बार यह बताया जाता है कि वह ‘कमज़ोर’, ‘निर्भर’, ‘त्यागी’ और ‘नरम दिल’ है, तो उसका मानसिक विकास उसी रूप में ढलने लगता है। बावजूद उसकी जैविक समानता के, उसके आत्मविश्वास को तोड़ा जाता है।
गिल्ट और शर्म: महिलाओं को अपनी इच्छाओं के लिए शर्मिंदा किया जाता है।
आत्म-संशय: कई स्त्रियाँ स्वयं को योग्य या सक्षम मानने में झिझकती हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से यह सीखा होता है कि ‘तुमसे नहीं होगा’।
6. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कथन की प्रासंगिकता
आज भले ही महिलाएं शिक्षा, राजनीति, व्यवसाय, विज्ञान आदि में आगे बढ़ रही हों, फिर भी उनके सामाजिक निर्माण की प्रक्रिया रुकी नहीं है। नारी के ऊपर अपेक्षाओं का बोझ आज भी है।
कार्यक्षेत्र में बराबरी पाने के बावजूद उसे घरेलू ज़िम्मेदारियों का बोझ उठाना होता है।
विवाह, मातृत्व, सुंदरता आदि की अपेक्षाएं अब भी स्त्रियों पर थोपी जाती हैं।
सोशल मीडिया भी एक नया मंच बन गया है जहाँ स्त्रियों से “एक परफेक्ट इमेज” की उम्मीद की जाती है।
6.1 कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव
आज भी कार्यस्थलों पर महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन, कम पदोन्नति और अधिक यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। स्त्रियों को “अंदरूनी” कामों के लिए उपयुक्त माना जाता है, जबकि पुरुषों को “बाहरी” और “नेतृत्वकारी” भूमिकाओं में।
6.2 घरेलू स्त्री की पहचान और मूल्यांकन
जो महिलाएं घर में रहकर परिवार का पालन-पोषण करती हैं, उन्हें समाज “कामकाजी” नहीं मानता। यह वही समाज है जिसने स्त्रियों के लिए यह भूमिका निर्धारित की – और फिर उसी को मूल्यहीन बना दिया।
6.3 विवाह और मातृत्व से जुड़ी सामाजिक अपेक्षाएं
कई समाजों में विवाह को स्त्री का “अंतिम लक्ष्य” माना जाता है। अविवाहित, तलाकशुदा या संतानहीन महिलाओं को संदेह या दया की दृष्टि से देखा जाता है – मानो वह ‘पूर्ण स्त्री’ न हों। यह सोच इस तथ्य को रेखांकित करती है कि स्त्रीत्व एक जैविक नहीं, बल्कि सामाजिक परिकल्पना है।
7. स्त्री विमर्श में इस कथन का योगदान
यह कथन स्त्री विमर्श की आधारशिला बन गया। इससे प्रेरित होकर कई विचारकों और आंदोलनकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि स्त्री की मुक्ति उसकी सामाजिक भूमिका के पुनर्निर्माण में है।
महत्वपूर्ण प्रभाव: स्त्री के लिए स्वतंत्रता, समानता और पहचान की मांग तेज़ हुई Feminist Epistemology, Gender Studies, और Intersectional Feminism जैसे विचार इसी सिद्धांत की जड़ों से निकले।
8. भारतीय संदर्भ में कथन का मूल्यांकन
भारतीय समाज में पितृसत्ता की जड़ें और गहरी हैं। यहाँ एक स्त्री के लिए “अच्छी बेटी”, “अच्छी बहू”, “अच्छी पत्नी” जैसी भूमिकाएँ पहले से परिभाषित हैं। भारतीय समाज में इसके उदाहरण:
बालिकाओं की शिक्षा को आज भी कई जगह गौण समझा जाता है। विवाह पूर्व स्त्री की स्वतंत्रता और बाद में उसकी आज़ादी पर कई प्रकार की सामाजिक पाबंदियाँ होती हैं। हालांकि कई महिलाएं अब इन बाधाओं को तोड़ रही हैं, फिर भी बहुसंख्यक स्त्रियां आज भी सामाजिक निर्माण की शिकार हैं।
9. नई चुनौतियाँ: तकनीक, पहचान और परिवर्तनशील स्त्रीत्व
9.1 सोशल मीडिया और ‘आदर्श स्त्री’ का डिजिटल संस्करण
इंस्टाग्राम, टिकटॉक और अन्य सोशल मीडिया मंचों ने स्त्रियों के लिए एक नया आदर्श गढ़ा है – “स्लिम, फेयर, ग्लैमरस, फिट, कुकिंग एक्सपर्ट, मदर-कम-इन्फ्लुएंसर।” स्त्रीत्व का यह नया अवतार भी एक बाह्य दबाव है – स्वनिर्मित नहीं, बल्कि “लाइक” और “फॉलोअर्स” आधारित।
9.2 ट्रांसजेंडर और नॉन-बाइनरी पहचानों का उभार
यह बोउवार के कथन को और बल देता है कि लिंग और लिंग-पर आधारित पहचानें (gender identities) जैविक नहीं होतीं। समाज की बनायी परिभाषाओं से परे जाकर, कई लोग अब खुद को स्त्री/पुरुष/अन्य रूपों में व्यक्त कर रहे हैं – जो सामाजिक निर्माणवाद की पुष्टि है।
संभावनाएं: शिक्षा, डिजिटल साक्षरता, सामाजिक आंदोलनों और महिला नेतृत्व के माध्यम से इस सोच को बदला जा सकता है। नई पीढ़ी की लड़कियाँ ‘स्त्री’ को एक नई परिभाषा देने की दिशा में अग्रसर हैं।
10. भारत में स्त्री का सामाजिक निर्माण: एक विश्लेषण
10.1 जाति और स्त्रीत्व का द्वंद्व
भारत में स्त्री की सामाजिक स्थिति जातिगत संरचनाओं से भी गहराई से जुड़ी है। एक दलित स्त्री और एक सवर्ण स्त्री के अनुभव अलग होते हैं – दोनों को “स्त्री” के रूप में समान नहीं देखा जाता। दलित स्त्रियों का स्त्रीत्व दोहरी मार झेलता है – जाति और लिंग की।
10.2 ग्रामीण बनाम शहरी स्त्री
शहरी महिलाओं को शिक्षा, आज़ादी और आत्मनिर्णय के अवसर अधिक मिलते हैं। परंतु ग्रामीण भारत में आज भी स्त्रियों को परदा प्रथा, बाल विवाह, दहेज और घरेलू हिंसा जैसी सामाजिक रूढ़ियों का सामना करना पड़ता है।
10.3 धर्म और स्त्रीत्व
धार्मिक परंपराओं में स्त्री को पूजनीय देवी और सेविका दोनों के रूप में प्रस्तुत किया गया है – एक ओर “काली,” “दुर्गा,” “सरस्वती” की शक्ति, तो दूसरी ओर “सीता,” “सावित्री,” “अनसूया” की पतिव्रता। यह द्वैत स्वयं में स्त्री की भूमिका को भ्रमित करता है।
11. संभावनाएं और परिवर्तन की राह
6.1 शिक्षा और आत्मनिर्भरता
जब महिलाएं शिक्षा के माध्यम से खुद को समझती हैं, वे अपने भीतर छिपी सामाजिक रूप से आरोपित ‘स्त्रीत्व’ की परतों को पहचानने लगती हैं। आत्मनिर्भरता स्त्री को पारंपरिक बंधनों से मुक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
11.2 पुरुषों की भूमिका
बोउवार के कथन के यथार्थ को केवल स्त्रियों का मुद्दा मानना एक भूल होगी। जब तक पुरुष भी अपनी ‘पौरुष’ की परिभाषा को पुनः परखेंगे नहीं, तब तक स्त्रीत्व की स्वतंत्र व्याख्या संभव नहीं। पितृसत्ता के खांचे में पुरुष भी बंधे हैं।
11.3 स्त्रीवाद की नई पीढ़ी
नवीन स्त्रीवादी आंदोलनों – जैसे #MeToo, #PinjraTod, #GirlsAtDhabas – यह दर्शाते हैं कि स्त्रियाँ अब अपने लिए “परिभाषाएं” नहीं, “चयन” चाहती हैं। वे तय करना चाहती हैं कि उन्हें क्या पहनना, पढ़ना, बोलना, करना और बनना है।
12. निष्कर्ष: स्त्री निर्माण को पुनर्संयोजन की आवश्यकता
सिमोन द बोउवार का यह कथन हमें केवल स्त्री की पीड़ा नहीं, बल्कि मुक्ति का रास्ता भी दिखाता है। आज की आवश्यकता है कि स्त्री को स्वतंत्र रूप से विकसित होने का अवसर देना। सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रीति-रिवाजों को पुनर्मूल्यांकित करना। स्त्री के आत्म-निर्माण को प्रोत्साहित करना – जिससे वह अपनी पहचान स्वयं तय कर सके, न कि समाज के निर्देशों से
सिमोन द बोउवार का कथन – “स्त्री पैदा नहीं होती, बनायी जाती है” – केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि लैंगिक विमर्श की नींव है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी स्त्री और पुरुष की धारणाएं, हमारी संस्कृति, भाषा, धर्म और राजनीति द्वारा गढ़ी गई हैं।
वर्तमान युग में, जब स्त्री शिक्षा प्राप्त कर रही है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही है, समाज में नेतृत्वकारी भूमिकाएं निभा रही है, तब यह कथन और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है। यह कथन हमें यह समझने की प्रेरणा देता है कि स्त्री होने का अर्थ जैविक नहीं, बल्कि चयन, आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है।
अतः आज आवश्यकता है कि स्त्री और पुरुष दोनों इस सामाजिक निर्माण को पहचानें, तोड़ें और मिलकर एक ऐसे समाज की स्थापना करें जहाँ कोई ‘बनाया’ न जाए – बल्कि हर व्यक्ति को खुद को ‘बनाने’ की पूरी आज़ादी हो।

डॉ प्रमोद कुमार
डिप्टी नोडल अधिकारी, MyGov
डॉ भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा