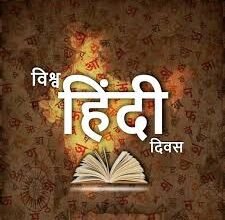भारत की गंगा-जमुनी तहज़ीब उसकी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह परंपरा सदियों से हिंदू-मुस्लिम-सिख-ईसाई सभी समुदायों के बीच सौहार्द, भाईचारे और एकता को बढ़ावा देती आई है। भारतीय समाज में विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं का संगम देखने को मिलता है, जो देश की अखंडता और संप्रभुता को सुदृढ़ करता है। गंगा-जमुनी तहज़ीब भारतीय संस्कृति की एक अनूठी पहचान है, जो विविधता में एकता की भावना को प्रकट करती है। यह केवल दो नदियों, गंगा और यमुना, के संगम का प्रतीक नहीं, बल्कि विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं के अद्भुत मेल का द्योतक है। भारत में सदियों से हिंदू-मुस्लिम, सिख-ईसाई सहित सभी समुदायों ने परस्पर सहयोग और सौहार्द के साथ जीवन व्यतीत किया है, जिससे यह तहज़ीब अस्तित्व में आई। यह लेख इस तहज़ीब के महत्व को विभिन्न दृष्टिकोणों से प्रस्तुत करेगा। यह लेख इस तहज़ीब के महत्व, उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, सामाजिक समरसता में भूमिका और वर्तमान समय की प्रासंगिकता पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालेगा।
गंगा-जमुनी तहज़ीब का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
गंगा-जमुनी तहज़ीब का उद्गम भारत की प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास में देखा जा सकता है। जब मुग़ल साम्राज्य भारत में आया, तब हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के मेलजोल से एक अनोखी सांस्कृतिक विरासत विकसित हुई। मुग़लकाल में संगीत, स्थापत्य कला, साहित्य, खान-पान और पहनावे में इस तहज़ीब की झलक देखने को मिली। अमीर खुसरो जैसे कवियों ने इस मिश्रण को अपनी कविताओं और संगीत के माध्यम से प्रकट किया। भक्तिकाल और सूफी आंदोलन ने भी इस तहज़ीब को मजबूत किया। कबीर, तुलसीदास, रसखान, बुल्ले शाह और बाबा फरीद जैसे संतों ने प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। इनके विचारों ने समाज में धार्मिक सद्भाव को बढ़ाया और यह भावना जनमानस में गहराई से स्थापित हो गई।
सामाजिक समरसता में गंगा-जमुनी तहज़ीब की भूमिका
यह तहज़ीब केवल धर्मों के मेल का प्रतीक नहीं, बल्कि सामाजिक ताने-बाने को भी मज़बूत करने वाला तत्व है। भारत जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र में यह सहिष्णुता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देती है। इसका प्रभाव निम्नलिखित क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है:
साहित्य और कला: भारतीय साहित्य और कला में इस तहज़ीब की गहरी छाप है। उर्दू साहित्य, हिंदी कविता, लोककथाएँ और विभिन्न भाषाओं में लिखी गई रचनाएँ इस मिश्रण को दर्शाती हैं। रामायण और महाभारत की कहानियाँ भी उर्दू में लिखी गईं, जबकि इस्लामी परंपराओं की कहानियाँ हिंदी और अन्य भाषाओं में समाहित हुईं।
संगीत और नृत्य: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, जिसमें ख्याल, ठुमरी, ग़ज़ल और कव्वाली शामिल हैं, इस तहज़ीब की देन हैं। नृत्य शैलियों में भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। कथक नृत्य शैली इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है।
खान-पान और पहनावा: भारतीय व्यंजन और परिधान भी इस तहज़ीब से प्रभावित हैं। बिरयानी, कबाब, कचौड़ी, समोसा, जलेबी जैसे खाद्य पदार्थ इसी मेल का परिणाम हैं। वहीं, शेरवानी, कुर्ता-पाजामा और साड़ी जैसी पोशाकें भी इस सांस्कृतिक संगम को दर्शाती हैं।
त्योहार और परंपराएँ: भारत में हिंदू-मुस्लिम एकता के उदाहरण के रूप में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। दीवाली, ईद, होली, बैसाखी, क्रिसमस और अन्य पर्वों को मिल-जुलकर मनाने की परंपरा इस तहज़ीब की खूबसूरती को दर्शाती है।
गंगा-जमुनी की विशेषताएँ
गंगा-जमुनी तहज़ीब भारत की मिश्रित सांस्कृतिक धरोहर है, जो विभिन्न धर्मों, भाषाओं, परंपराओं और रीति-रिवाजों के मेल से बनी है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं:
सांस्कृतिक समन्वय– यह तहज़ीब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य धर्मों की परंपराओं का संगम है, जिससे सामाजिक सौहार्द और मेलजोल को बढ़ावा मिलता है।
भाषा और साहित्य– हिंदी, उर्दू, अवधी, ब्रजभाषा जैसी भाषाओं का आपसी समन्वय इस तहज़ीब की विशेषता है। उर्दू शायरी और हिंदी कविताओं में इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है।
कला और संगीत– भारतीय शास्त्रीय संगीत, विशेष रूप से ख्याल, ठुमरी, ग़ज़ल और कव्वाली, इस तहज़ीब का हिस्सा हैं। कथक नृत्य शैली भी इसी सांस्कृतिक समन्वय का उदाहरण है।
खान-पान– भारतीय भोजन में भी गंगा-जमुनी तहज़ीब की झलक मिलती है। बिरयानी, कबाब, समोसा, जलेबी, कचौड़ी जैसी व्यंजन परंपराएँ इसी का परिणाम हैं।
त्योहारों का समावेश– दीपावली, ईद, होली, बैसाखी, क्रिसमस जैसे त्योहारों को सभी समुदायों द्वारा मिल-जुलकर मनाना इस तहज़ीब की खूबसूरती को दर्शाता है।
समाज में आपसी सद्भाव– यह तहज़ीब सहिष्णुता, प्रेम, भाईचारे और सौहार्द का संदेश देती है, जिससे भारत की एकता और अखंडता मजबूत होती है।
वेशभूषा और परंपराएँ– शेरवानी, कुर्ता-पायजामा, साड़ी, दुपट्टा जैसी पारंपरिक पोशाकें इस तहज़ीब के प्रभाव को दर्शाती हैं।
धर्मनिरपेक्षता का समर्थन– यह तहज़ीब सभी धर्मों के प्रति सम्मान और समानता की भावना को प्रोत्साहित करती है, जिससे भारत की धर्मनिरपेक्षता मजबूत होती है।
लोक संस्कृति और परंपराएँ– विवाह, संगीत, नृत्य और सामाजिक रीति-रिवाजों में भी हिंदू-मुस्लिम संस्कृति का समावेश देखा जाता है, जो तहज़ीब की प्रमुख विशेषताओं में से एक है।
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में गंगा-जमुनी तहज़ीब का महत्व
गंगा-जमुनी तहज़ीब का उद्भव भारत के प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास से जुड़ा हुआ है। मुग़ल काल में इस सांस्कृतिक समन्वय को बल मिला, जब कला, साहित्य, संगीत, और खान-पान में हिंदू और मुस्लिम परंपराओं का समावेश हुआ। अमीर खुसरो, रसखान, कबीर, तुलसीदास और अन्य संत कवियों ने इस मिश्रण को अपने साहित्य और संगीत में दर्शाया। इस तहज़ीब ने समाज में समरसता और परस्पर सम्मान की भावना को बढ़ावा दिया।
सामाजिक सद्भाव में योगदान
1. धार्मिक सौहार्द– गंगा-जमुनी तहज़ीब ने विभिन्न धर्मों के लोगों को एक मंच पर लाकर परस्पर सहयोग और सौहार्द का वातावरण तैयार किया।
2. भाषाई समन्वय– हिंदी, उर्दू, अवधी, ब्रज जैसी भाषाओं में इस तहज़ीब की झलक मिलती है। उर्दू और हिंदी साहित्य में धार्मिक और सामाजिक एकता को प्रमुखता दी गई है।
3. त्योहारों का मेल– ईद, दिवाली, होली, बैसाखी, क्रिसमस आदि त्योहारों को सभी समुदायों द्वारा मिल-जुलकर मनाना इसकी प्रमुख विशेषता है।
कला, संगीत और साहित्य में योगदान
1. संगीत– हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, विशेष रूप से ख्याल, ठुमरी, कव्वाली और ग़ज़ल, इसी तहज़ीब की देन हैं।
2. नृत्य– कथक नृत्य शैली में हिंदू और मुस्लिम दोनों परंपराओं का मिश्रण मिलता है।
3. साहित्य– हिंदी-उर्दू साहित्य में गंगा-जमुनी तहज़ीब की भावना स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। तुलसीदास और कबीर के दोहों से लेकर मीर, ग़ालिब और प्रेमचंद की रचनाओं तक इस तहज़ीब का प्रभाव बना रहा।
राष्ट्रीय अखंडता, संप्रभुता और एकता में गंगा-जमुनी तहज़ीब का योगदान
भारत की एकता और अखंडता में गंगा-जमुनी तहज़ीब का बहुत बड़ा योगदान है। यह तहज़ीब विविधता में एकता की भावना को प्रबल करती है और सभी धर्मों और समुदायों को आपसी सौहार्द्र के सूत्र में पिरोती है।
धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा: भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता को अपनाता है, और गंगा-जमुनी तहज़ीब इस विचारधारा को बल प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करती है कि सभी धर्म समान रूप से सम्मानित हों और किसी भी समुदाय को अन्य पर श्रेष्ठता न दी जाए।
सामाजिक एकता: जब समाज में सांप्रदायिक सौहार्द्र बना रहता है, तो राष्ट्र की एकता स्वतः ही सुदृढ़ होती है। गंगा-जमुनी तहज़ीब भारत के लोगों को एक-दूसरे से जोड़ती है और सांप्रदायिक तनाव को कम करने में सहायक होती है।
आर्थिक और सांस्कृतिक विकास: इस तहज़ीब ने देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान दिया है। हस्तशिल्प, संगीत, सिनेमा, खान-पान, और पर्यटन उद्योग इसकी वजह से फले-फूले हैं। भारतीय फिल्म उद्योग में भी इस तहज़ीब का व्यापक प्रभाव देखा जाता है।
लोकतंत्र की मजबूती: जब विभिन्न समुदायों के लोग एकता और समरसता के साथ रहते हैं, तो लोकतंत्र मजबूत होता है। यह तहज़ीब सभी जातियों और धर्मों के बीच परस्पर सम्मान और सह-अस्तित्व को बढ़ावा देती है, जिससे देश की संप्रभुता सुदृढ़ होती है।
वर्तमान समय में गंगा-जमुनी तहज़ीब की प्रासंगिकता
आज के समय में जब वैश्वीकरण, सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक मतभेद बढ़ रहे हैं, तब गंगा-जमुनी तहज़ीब की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है। यह तहज़ीब हमें आपसी प्रेम, सहयोग और समरसता का संदेश देती है, जिससे समाज में नफरत और विभाजन की राजनीति का प्रभाव कम किया जा सकता है। सरकार और समाज को मिलकर इस तहज़ीब को बचाने और बढ़ावा देने के प्रयास करने चाहिए। शैक्षिक पाठ्यक्रमों में इस संस्कृति को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी इसकी महत्ता को समझ सके। साथ ही, साहित्य, कला, संगीत और फिल्म उद्योग को भी इस तहज़ीब को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करना चाहिए। आज के समय में जब समाज में सांप्रदायिक तनाव और विघटन की प्रवृत्तियाँ देखी जाती हैं, गंगा-जमुनी तहज़ीब की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।
गंगा-जमुनी तहज़ीब भारत की आत्मा है। यह सदियों से देश की अखंडता, संप्रभुता और एकता को बनाए रखने में सहायक रही है। यह केवल दो नदियों के मेल का प्रतीक नहीं, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और परंपराओं के अद्भुत संगम का प्रतीक है। यह केवल एक सांस्कृतिक अवधारणा नहीं, बल्कि सामाजिक एकता, धार्मिक सौहार्द और राष्ट्रीय अखंडता की नींव भी है। इसे संरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि भारत की सांस्कृतिक धरोहर सशक्त बनी रहे और भविष्य में भी सामाजिक समरसता और सौहार्द को बढ़ावा मिले।
इस तहज़ीब को सहेजकर रखना न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करना है, बल्कि भारत की संप्रभुता और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती प्रदान करना भी है।

डॉ प्रमोद कुमार
डिप्टी नोडल अधिकारी, MyGov
डॉ भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा