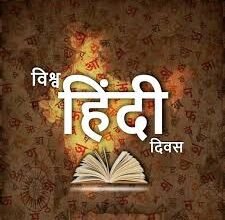“शिक्षा का बदलता परिदृश्य और जनमानस की असमंजसता: विकसित भारत के राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में निजीकरण और सरकारी व्यवस्था का द्वंद्व”
डॉ प्रमोद कुमार

भारत में शिक्षा केवल ज्ञानार्जन का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और राष्ट्र निर्माण का आधार रही है। यह वह सशक्त माध्यम है जो व्यक्ति को जागरूक नागरिक और सशक्त मानव संसाधन में परिवर्तित करता है। इसी दृष्टिकोण से देश में समय-समय पर शिक्षा नीतियों का निर्माण हुआ है। वर्ष 2020 में लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020), 34 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद प्रस्तुत एक क्रांतिकारी दस्तावेज है, जिसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों के अनुरूप, समावेशी, लचीली, बहुभाषिक और बहुआयामी बनाना है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP-2020) को इस उद्देश्य से लाया गया कि यह भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, समावेशी और समकालीन बनाए। किंतु इसके लागू होने के साथ ही निजीकरण और सरकारी शिक्षा व्यवस्था के बीच एक तीव्र द्वंद्व पैदा हो गया है। इस द्वंद्व में आम जनता, विशेषकर निम्न और मध्यम वर्गीय जनमानस, असमंजस की स्थिति में फंसा हुआ है। हालाँकि, इस नीति के क्रियान्वयन में निजीकरण और सरकारी व्यवस्था के बीच जो द्वंद्व उभरकर सामने आया है, उसने जनमानस, विशेषतः ग्रामीण, निम्न एवं मध्यम वर्गीय समाज को असमंजस की स्थिति में ला खड़ा किया है। एक ओर निजी संस्थानों को बढ़ावा देने, स्वायत्तता देने और डिजिटल माध्यमों के उपयोग को प्राथमिकता दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों में संसाधनों की कमी, शिक्षकों की अनुपलब्धता और नीति की धीमी क्रियान्वयन गति गंभीर प्रश्न खड़े करती है।
इस द्वंद्वात्मक स्थिति में आम नागरिक यह समझ नहीं पा रहा कि बदलते शिक्षा परिदृश्य में उसका स्थान क्या है, और उसके बच्चों का भविष्य किस दिशा में अग्रसर होगा। प्रस्तुत लेख इसी द्वंद्व का गहन विश्लेषण करते हुए यह समझने का प्रयास करता है कि कैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का क्रियान्वयन शिक्षा को समावेशी बनाने के बजाय कहीं उसे विशिष्ट वर्गों तक सीमित करने का माध्यम तो नहीं बन रहा है। यह लेख इस द्वंद्वात्मक स्थिति की गहराई से समीक्षा करता है और यह स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि कैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में निजीकरण और सरकारी शिक्षा के बीच का संतुलन असमान रूप से बिगड़ता प्रतीत होता है।
1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का संक्षिप्त परिचय:
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, 34 वर्षों बाद लाई गई एक नई नीति है, जिसने भारत की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन का वादा किया। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं:
समग्र और बहुआयामी शिक्षा प्रणाली की स्थापना
मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान
लचीला पाठ्यक्रम और बहुविषयक दृष्टिकोण
उच्च शिक्षा में स्वायत्तता और मूल्यांकन की पारदर्शिता
डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास पर बल
इन उद्देश्यों के पीछे शिक्षा की गुणवत्ता और व्यावसायिक उपयोगिता को केंद्र में लाने का प्रयास स्पष्ट होता है, लेकिन जब इस नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हुई तो निजीकरण की प्रवृत्ति और सरकारी शिक्षा संस्थानों की उपेक्षा के आरोप लगने लगे।
2. निजीकरण की प्रवृत्ति और शिक्षा में उसका प्रभाव:
निजीकरण का अर्थ है शिक्षा प्रणाली में निजी संस्थाओं, कॉर्पोरेट घरानों और निजी पूंजी निवेश को बढ़ावा देना। शिक्षा नीति 2020 के कुछ बिंदु:
निजी उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वायत्तता
ऑनलाइन शिक्षा में निजी प्लेटफार्मों की भागीदारी
PPP मॉडल (Public-Private Partnership) को प्रोत्साहन
इन पहलुओं ने शिक्षा को एक सेवा (service) के बजाय एक ‘उत्पाद’ (commodity) के रूप में प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। इससे शिक्षा का व्यवसायीकरण बढ़ा है, जिससे आम नागरिक, विशेषतः ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वयं को पीछे छूटा महसूस कर रहा है।
3. सरकारी शिक्षा व्यवस्था की स्थिति और चुनौतियाँ:
सरकारी शिक्षा व्यवस्था का भारत के ग्रामीण और अर्ध-शहरी समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यह वह आधार है, जिस पर करोड़ों विद्यार्थियों की शैक्षिक आकांक्षाएं टिकी रहती हैं, विशेषकर उन परिवारों की जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन के बाद यह चिंता गहराई है कि सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों की नही उपेक्षा की जा रही है।
मुख्य चुनौतियाँ:
बुनियादी ढांचे की कमी: सरकारी विद्यालयों में शौचालय, पीने का पानी, पुस्तकालय, डिजिटल सुविधाएं आदि का भारी अभाव है।
शिक्षकों की कमी और प्रशिक्षण: योग्य शिक्षकों की भर्ती न होना और नियुक्त शिक्षकों का नियमित प्रशिक्षण न होना।
पाठ्यक्रम में जमीनी हकीकत से दूरी: नीति के अनुसार बदलाव तो किए गए, लेकिन उनका ज़मीनी अनुप्रयोग अत्यंत सीमित है।
अवसरों की असमानता: शिक्षा में निजी संस्थानों की बढ़ती प्रधानता से सरकारी छात्रों के लिए प्रतियोगी अवसर और रोजगार की राह कठिन होती जा रही है।
जब सरकारी शिक्षा में संसाधन नहीं बढ़ते, बल्कि निजीकरण को बल मिलता है, तब जनमानस का असमंजस गहराता है – क्या सरकारी संस्थान भविष्य में जीवित रहेंगे या केवल एक औपचारिक ढांचा बनकर रह जाएंगे?
4. शिक्षा में असमानता की खाई:
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 समावेशिता और समता की बात करती है, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से यह देखा जा रहा है कि—
निजी संस्थान शुल्क में अत्यधिक वृद्धि कर रहे हैं, जो आम नागरिक की पहुंच से बाहर है।
शहरी और ग्रामीण शिक्षा के बीच की खाई और अधिक चौड़ी हो गई है।
डिजिटल डिवाइड यानी इंटरनेट, स्मार्टफोन और लैपटॉप की अनुपलब्धता ने ग्रामीण और निर्धन छात्रों को पीछे धकेल दिया है।
शिक्षा के क्षेत्र में यह खाई केवल आर्थिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी गहरी हो रही है, जिससे समतामूलक समाज का सपना अधूरा रह जाता है।
5. जनमानस का असमंजस और बढ़ती असुरक्षा:
शिक्षा नीति के प्रचार में यह दिखाया गया कि यह नीति छात्रों के हित में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, लेकिन व्यवहार में:
माता-पिता समझ नहीं पा रहे कि कौन-सा विकल्प बेहतर है – निजी या सरकारी?
छात्र भ्रमित हैं कि उनके द्वारा प्राप्त डिग्री और कौशल की प्रासंगिकता भविष्य में कितनी उपयोगी होगी।
शिक्षक समुदाय आशंकित है कि कहीं उनकी भूमिका सीमित न हो जाए या नौकरी असुरक्षित न बन जाए।
इस असमंजस की स्थिति से एक बड़ा वर्ग मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और व्यावसायिक अनिश्चितता का शिकार हो रहा है, जो शिक्षा की आत्मा को ही क्षत-विक्षत करता है।
6. शिक्षा का बाजारीकरण: एक नैतिक संकट:
जब शिक्षा को एक वस्तु के रूप में देखा जाता है, तो उसमें मूल्यों का ह्रास अवश्यंभावी हो जाता है। निजीकरण की आड़ में शिक्षा:
लाभ कमाने का साधन बन जाती है, जहाँ गुणवत्ता और मूल्य गौण हो जाते हैं।
नैतिकता और करुणा जैसे मूलभूत शैक्षिक आदर्श गुम हो जाते हैं।
शिक्षा संस्थानों में प्रतिस्पर्धा की जगह मुनाफे की होड़ लग जाती है।
इससे शिक्षा अपने मानव निर्माण के ध्येय से भटककर केवल कौशल निर्माण या रोजगार-केन्द्रित प्रणाली बन जाती है, जो समाज के दीर्घकालिक विकास के लिए घातक हो सकती है।
7. डिजिटल शिक्षा: अवसर या विस्थापन?
NEP-2020 में डिजिटल शिक्षा को व्यापक रूप से बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसके तहत:
ऑनलाइन कोर्स, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, वर्चुअल प्रयोगशाला आदि की घोषणा की गई।
स्वयं, दीक्षा जैसे सरकारी प्लेटफॉर्म विकसित किए गए।
लेकिन ज़मीनी स्तर पर डिजिटल संसाधनों की असमान उपलब्धता ने निम्न और मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों को कठिनाई में डाल दिया:
60% से अधिक ग्रामीण विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं हैं।
इंटरनेट की गति और लागत एक बड़ी बाधा है।
डिजिटल माध्यम में शिक्षक-छात्र संबंध और संवाद की गुणवत्ता क्षीण हो जाती है।
इस प्रकार डिजिटल शिक्षा एक ओर अवसर है, लेकिन जब तक डिजिटल समानता स्थापित नहीं होती, तब तक यह एक बड़ा विस्थापन भी है।
8. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सुधार की संभावनाएँ:
नीति के अंतर्निहित उद्देश्य सकारात्मक हैं, किंतु उन्हें समावेशिता, समानता और जनहित की दृष्टि से लागू करना अनिवार्य है:
सरकारी शिक्षा में निवेश और सुधार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
निजी संस्थानों के लिए शुल्क निर्धारण की पारदर्शी प्रणाली लागू होनी चाहिए।
डिजिटल शिक्षा के साथ-साथ भौतिक शिक्षण का संतुलन बनाया जाए।
जनभागीदारी और शिक्षक समुदाय की राय को नीति निर्धारण में स्थान मिले।
यदि इन बातों को ध्यान में रखते हुए NEP को क्रियान्वित किया जाए, तो यह नीति भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में सहायक सिद्ध हो सकती है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भारत की शैक्षिक संरचना में एक ऐतिहासिक कदम है, किंतु इसके क्रियान्वयन में निजीकरण और सरकारी व्यवस्था के बीच जो द्वंद्व उत्पन्न हुआ है, वह अत्यंत विचारणीय है। आम जनमानस विशेषतः निम्न और मध्यम वर्गीय नागरिक इस परिवर्तनशील दौर में असमंजस की स्थिति में हैं, जहाँ उन्हें यह निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है कि कौन-सी दिशा उनके बच्चों के भविष्य के लिए उचित है। यदि शिक्षा को समावेशी, न्यायसंगत और नैतिक बनाना है तो निजी और सरकारी व्यवस्था के बीच संतुलन बनाना होगा, ताकि शिक्षा एक अधिकार, एक अवसर और एक सामाजिक उत्तरदायित्व बनी रहे – न कि केवल लाभ आधारित सेवा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 एक ऐतिहासिक प्रयास है जो भारतीय शिक्षा प्रणाली को समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने की दिशा में उठाया गया महत्त्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य समावेशी, बहुआयामी, कौशल-आधारित और मातृभाषा-समर्थित शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देना है। किंतु इसके लागू होने के साथ ही शिक्षा के निजीकरण और सरकारी संस्थानों की उपेक्षा को लेकर जो द्वंद्व उत्पन्न हुआ है, वह जनमानस को भ्रम और असमंजस की स्थिति में डाल रहा है।
नीति के कई बिंदु, जैसे डिजिटल शिक्षा, बहुभाषिकता और बहु-विषयक दृष्टिकोण, यथार्थ में सामाजिक और आर्थिक असमानता को और गहरा करते दिख रहे हैं। निजी संस्थानों की बढ़ती भूमिका ने शिक्षा को ‘अधिकार’ से अधिक एक ‘उत्पाद’ बना दिया है, जिससे निम्न और मध्यम वर्गीय वर्ग स्वयं को पीछे छूटा हुआ महसूस करता है। दूसरी ओर, सरकारी संस्थानों में बुनियादी संसाधनों की कमी, शिक्षकों की अनुपलब्धता और नीति क्रियान्वयन की धीमी गति ने जनता के विश्वास को डगमगाया है।
आज शिक्षा केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, आर्थिक अवसर और नैतिक जागरूकता की आधारशिला है। ऐसे में यदि शिक्षा व्यवस्था ही वर्गभेद और अवसरहीनता को जन्म देने लगे, तो विकसित भारत का सपना अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि नीति में निजी और सरकारी प्रणाली के बीच संतुलन स्थापित किया जाए, डिजिटल और भौतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो, और सबसे बढ़कर – शिक्षा को लाभ का नहीं, सेवा और अधिकार का माध्यम माना जाए। तभी जनमानस का असमंजस दूर होगा और भारत शिक्षा के माध्यम से सच में विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हो सकेगा।
डॉ प्रमोद कुमार
डिप्टी नोडल अधिकारी, MyGov
डॉ भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा